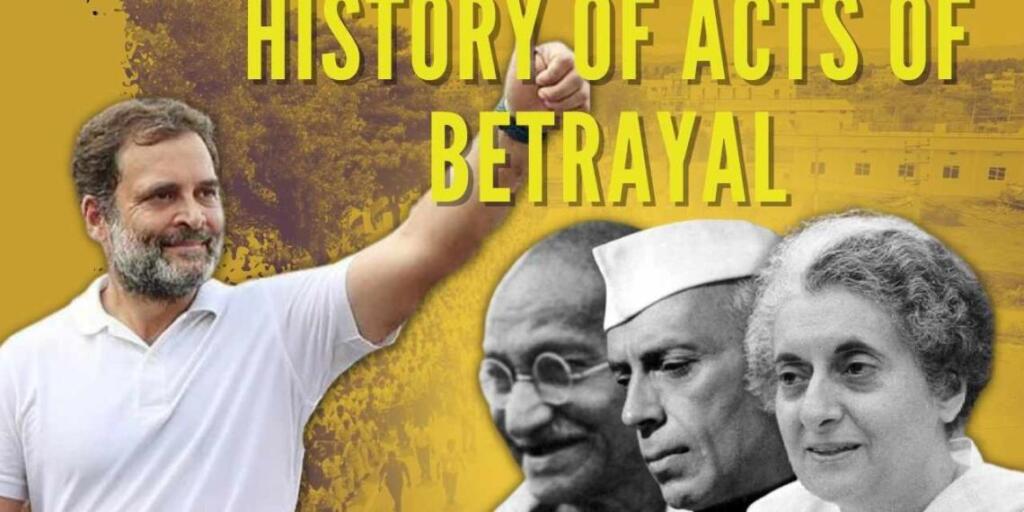1947 के बाद कांग्रेस ने भारत की शिक्षा व्यवस्था, मीडिया और सांस्कृतिक संस्थाओं पर पूरा नियंत्रण जमा लिया। इतिहास को इस तरह दोबारा लिखा गया कि उसमें केवल उसके राजनीतिक नेताओं की महिमा गाई गई-लेकिन उन सैनिकों का जिक्र बहुत कम हुआ जिन्होंने अपनी जानें देकर इस देश की सीमाएँ सुरक्षित रखीं।
भारत का सैन्य इतिहास साहस, त्याग और मौन सहनशीलता की एक अद्भुत गाथा है। लेकिन, अगर आप कांग्रेस के बनाए इतिहास की किताबें पढ़ेंगे, तो आपको यह कभी महसूस नहीं होगा। जिस पल कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत की छाया में राजनीतिक उभार पाया, उसी पल से उसने भारत की सशस्त्र शक्ति को कमतर दिखाने की सोची-समझी रणनीति अपनाई। आज़ादी के बाद भी सात दशकों तक उसने हर सैन्य विजय को राजनीतिक प्रचार में बदल दिया, हर सैनिक की बहादुरी को नेताओं की फोटो-ऑप तक सीमित कर दिया और हर राष्ट्रीय रक्षा प्रयास को शक, व्यंग्य या भ्रष्टाचार से घेर दिया।
यह सब किसी संयोग का परिणाम नहीं था। यह एक गहरे वैचारिक डिज़ाइन का हिस्सा था, जो कांग्रेस की औपनिवेशिक उत्पत्ति से जन्मा, स्वतंत्र भारत में उसके असुरक्षा-बोध से पला और शिक्षा, मीडिया व नौकरशाही के बौद्धिक कब्जे के ज़रिए सशक्त हुआ।
औपनिवेशिक बीज: ऐसी पार्टी जो लड़ने नहीं, मनाने के लिए बनी थी
कांग्रेस पार्टी वास्तव में कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं थी। उसका जन्म ब्रिटिश अफ़सरों और अंग्रेज़ी शिक्षित भारतीय अभिजात वर्ग के बीच एक ड्रॉइंग रूम चर्चा मंच के रूप में हुआ था। एक ऐसा ‘राजनीतिक कुशन’ जिसे ब्रिटिश राज ने भारतीय असंतोष को नियंत्रण में रखने के लिए तैयार किया था, ताकि देशवासी हिंसक विद्रोह की जगह विनम्र निवेदन में उलझे रहें।
ब्रिटिश शासन की नींव भारतीयों की आज्ञाकारिता पर टिकी थी, विद्रोह पर नहीं। इसलिए 1857 के संग्राम से लेकर बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलनों तक और अंततः 1946 के नौसैनिक विद्रोह तक, हर सशस्त्र उठान न सिर्फ़ ब्रिटिश साम्राज्य बल्कि कांग्रेस की अपनी राजनीति के लिए भी खतरा था। ब्रिटिशों को यह भलीभांति पता था कि कांग्रेस उनके लिए उपयोगी है। वह जनता को ‘नियंत्रित असंतोष’ की सीमाओं में रखती है, जबकि असली विद्रोहियों को ब्रिटिश गोलियों से कुचल दिया जाता है।
विडंबना देखिए, यही कांग्रेस पार्टी प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटिशों के आदेश पर भारतीय सैनिकों को विदेशी धरती पर लड़ने भेजती रही, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य सुरक्षित रहे। पर जब वही सैनिक अपने ही देश को आज़ाद कराने के लिए हथियार उठाते, तो कांग्रेस उन्हें नैतिक रूप से तिरस्कृत करती।
यहीं से कांग्रेस की ‘सैन्य शक्ति’ के प्रति आजीवन एलर्जी शुरू हुई। भारतीय सैनिक, जो अनुशासित, निर्भीक, राष्ट्रभक्त और राजनीतिक दांव-पेंचों से ऊपर होता है। कांग्रेस की पूरी मानसिकता के लिए भय का प्रतीक बन गया। कांग्रेस के लिए स्वतंत्रता वह थी, जो कोट-पैंट पहने नेताओं की बातचीत से हासिल हो, न कि उन सैनिकों के रक्त से जो सरहदों पर लड़े।
नेहरू का भारत: अविश्वास, निरस्त्रीकरण और जानबूझकर की गई कमजोरी
जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब जवाहरलाल नेहरू ने केवल सत्ता ही नहीं संभाली, बल्कि उस औपनिवेशिक मानसिकता को भी विरासत में लिया, जिसमें सेना को शक की नज़र से देखा जाता था। उन्हें उस संस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं था जिसने भारत की सीमाओं के लिए रक्त बहाया था, बल्कि वे उससे डरते थे।
नेहरू के लिए एक मजबूत सेना उनके उस बौद्धिक और नैतिक भारत के सपने के लिए खतरा थी, जिसे वे अहिंसक, आदर्शवादी और विश्व नेता के रूप में पेश करना चाहते थे। वे भाषणों के ज़रिए विश्व का नेतृत्व करना चाहते थे, शक्ति के बल पर नहीं। उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा आदर्शवाद, दिखावटी बौद्धिकता और गांधीवादी अहिंसा के मिश्रण पर आधारित थी।
परिणामस्वरूप, सशस्त्र बलों को लगातार नज़रअंदाज़ किया गया, उनकी फंडिंग घटाई गई और उनकी रणनीति पर नौकरशाहों व तथाकथित बुद्धिजीवियों का कब्ज़ा हो गया। जिन लोगों ने कभी सीमा नहीं देखी, वे रक्षा नीति तय करने लगे और सैनिक नौकरशाही के अधीन हो गए। जब सैन्य विशेषज्ञों ने 1950 के दशक के अंत में चीन के खतरे की चेतावनी दी तो नेहरू ने उसका मज़ाक उड़ाया। उन्होंने यहां तक कहा कि जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता, वहां रक्षा चौकियां बनाने का क्या मतलब है।
पंडित नेहरू के इस अहंकार की भारी कीमत 1962 में भारतीय सैनिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हमारे वीर सैनिक, जिनके पास साहस था लेकिन उपकरण और राजनीतिक समर्थन नहीं, उन्हें असंगठित और असुरक्षित मोर्चे पर भेज दिया गया। परिणामस्वरूप भारत को आधुनिक इतिहास की सबसे अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी कांग्रेस ने आत्ममंथन नहीं किया। उसने हार से सीखने के बजाय उसे सरकारी गोपनीयता और शैक्षणिक झूठ के परतों में दबा दिया।
भूले हुए नायक: रेज़ांग ला से लेकर लॉन्गेवाला तक
1962 की पराजय के बाद भी भारत के सैनिकों ने अपने साहस और समर्पण से यह सिद्ध कर दिया कि देश की रक्षा केवल नेताओं के भाषणों से नहीं, बल्कि जवानों के खून-पसीने से होती है। मगर कांग्रेस की राजनीति ने उन बलिदानों को भी भुला दिया, जिनकी गूंज आज भी हिमालय की चोटियों और राजस्थान की रेत में सुनाई देती है।
रेज़ांग ला — यह नाम भारत के सैन्य इतिहास का प्रतीक है। पूर्वी लद्दाख की जमी हुई घाटी में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की ‘सी कंपनी’ के 120 जवानों ने चीनी सेना के सैकड़ों सैनिकों को रोकते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनके पास न तो पर्याप्त गोला-बारूद था, न रसद, न ही ऊनी कपड़े। लेकिन उन्होंने अपने देश की मिट्टी छोड़ने से इनकार कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब उनके शवों को उन्हीं मोर्चों पर पाया गया। हथियार हाथ में और निगाहें दुश्मन की दिशा की ओर।
लेकिन दिल्ली में बैठे नेताओं ने उनके बलिदान को इतिहास के पन्नों में दबा दिया। न तो संसद में कोई विस्तृत श्रद्धांजलि दी गई और न ही इतिहास की किताबों में उनका जिक्र। कांग्रेस की प्राथमिकता तब भी “अंतरराष्ट्रीय छवि” थी, न कि उन जवानों की वीरता जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए दिए।
1971 का युद्ध — जो भारत के गौरवशाली सैन्य अध्यायों में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। वह भी कांग्रेस की आत्ममुग्ध राजनीति की भेंट चढ़ गया। यह युद्ध भारतीय सेना की असाधारण योजना, रणनीति और साहस का परिणाम था। जनरल सैम मानेकशॉ जैसे महान सेनापति ने एक ऐसा अभियान चलाया, जिसने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यह भारत की निर्णायक सैन्य विजय थी। लेकिन, कांग्रेस ने इसे इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत जीत बना दिया।
देश के नायक सैम मानेकशॉ, जगजीत सिंह अरोड़ा और सैकड़ों वीर जवानों की जगह मीडिया और इतिहास में “इंदिरा इज इंडिया” का नारा गूंजा। यही वह क्षण था जब कांग्रेस ने सैन्य उपलब्धियों को राजनीतिक स्वामित्व में बदलने की परंपरा शुरू की। एक ऐसी परंपरा, जिसमें सैनिकों का पराक्रम नेताओं की महिमा के नीचे दब गया।
1971 के बाद भी कई बार भारतीय सेना ने अपना कौशल और वीरता सिद्ध की। चाहे 1965 में हाजी पीर और असल उत्तर सेक्टर में पाकिस्तानी टैंकों को धूल चटाना हो या 1999 में कारगिल की बर्फ़ीली चोटियों पर तिरंगा फहराना। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता वही रही, सेना की सफलता पर सियासत का रंग चढ़ाना और असफलता पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना।
इंदिरा गांधी और सैन्य सफलता का राजनीतिक दोहन
इंदिरा गांधी के दौर में भारतीय सेना ने कई निर्णायक अभियान चलाए, लेकिन हर सफलता को एक महिला नेता के लौह संकल्प की कहानी के रूप में पेश किया गया। जबकि सच्चाई यह थी कि 1971 का विजय अभियान पूरी तरह सेना की रणनीतिक तैयारी, सैनिकों की निष्ठा और खुफिया एजेंसियों के गुप्त समन्वय का नतीजा था।
इंदिरा गांधी ने उस विजय का उपयोग अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने में किया। उन्होंने सत्ता को और केंद्रीकृत किया, सेना पर राजनीतिक नियंत्रण और भी कस दिया, और जनरल मानेकशॉ जैसे ईमानदार सेनापतियों को धीरे-धीरे हाशिए पर डाल दिया।
1975 में आपातकाल लगाकर उन्होंने यह भी दिखा दिया कि कांग्रेस के लिए लोकतंत्र और सैन्य अनुशासन दोनों ही केवल उतने उपयोगी हैं, जितने तक वे सत्ता को बनाए रखने में सहायक हों। उस दौर में देश के भीतर सैनिक अनुशासन का प्रतीक “राष्ट्र के प्रति समर्पण” नहीं, बल्कि “सरकार के प्रति आज्ञाकारिता” बना दिया गया।
कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि सेना कभी स्वतंत्र विचारशील संस्था न बने। उसकी छवि को या तो “राष्ट्रवाद के खतरे” के रूप में पेश किया गया या फिर “राजनीतिक अधीनता” के प्रतीक के रूप में।
मीडिया और अकादमिक जगत में कांग्रेस की वैचारिक जंग
कांग्रेस को यह समझ थी कि जब तक सैनिक का सम्मान जनमानस में जीवित रहेगा, तब तक उसकी “नैरेटिव राजनीति” कमजोर पड़ेगी। इसलिए उसने शिक्षा, मीडिया और कला-संस्कृति के जरिए धीरे-धीरे एक नई मानसिक गुलामी पैदा की, जिसमें वीरता की जगह ‘विनम्रता’ और पराक्रम की जगह ‘प्रशासनिक शांति’ का महिमामंडन किया गया।
विद्यालयों में बच्चों को यह सिखाया गया कि भारत ने युद्ध नहीं, “शांति की राजनीति” से प्रगति की। फिल्मों और साहित्य में सैनिक को या तो भावुक पात्र के रूप में दिखाया गया या फिर “सत्ता के उपकरण” के तौर पर। जिन लेखकों ने सैनिक बलिदान की महिमा लिखनी चाही, उन्हें ‘मिलिटेंट नेशनलिस्ट’ कहकर अलग कर दिया गया। कांग्रेस के इस सांस्कृतिक नियंत्रण ने आने वाली पीढ़ियों के मन से यह भाव मिटा दिया कि राष्ट्र की रक्षा केवल विचारों से नहीं, बल्कि शक्ति और साहस से होती है।
कांग्रेस का वैचारिक तंत्र समझ चुका था कि अगर भारतीय समाज में सैनिक के प्रति सम्मान और सैन्य परंपरा का गौरव बना रहा, तो उसकी राजनीति की नींव कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए आज़ादी के बाद उसने योजनाबद्ध तरीके से इतिहास और समाजशास्त्र दोनों को हथियार बना लिया। स्कूलों की किताबों में सैनिकों का नाम घटा दिया गया, राष्ट्रीय आंदोलनों के उन वीरों का उल्लेख मिटा दिया गया जिन्होंने अंग्रेजों से सीधी लड़ाई लड़ी थी। 1857 के नायक मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस को या तो “हिंसक” कहा गया या “विचलित क्रांतिकारी” के रूप में पेश किया गया, जबकि अंग्रेजों से समझौता करने वाले नेताओं को “महात्मा” और “दूरदर्शी” का दर्जा दिया गया।
यह वही दौर था जब मीडिया और साहित्य में भी एक खास प्रकार की विचारधारा थोप दी गई, जहां सैनिक की वीरता को नहीं, बल्कि “अहिंसा” के नैतिक बोध को सर्वोच्च मानक बताया गया। फिल्मों में सैनिक का चरित्र या तो भावुक, टूटे हुए व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता या उसे सत्ता की मशीन का प्रतीक बना दिया जाता। धीरे-धीरे एक पूरी पीढ़ी ऐसी बनी जो अपने रक्षकों को श्रद्धा से नहीं, बल्कि दूरी से देखने लगी।
कांग्रेस के इस बौद्धिक कब्जे का दूसरा परिणाम यह हुआ कि सशस्त्र बलों की रणनीतिक स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई। रक्षा मंत्रालय पर नौकरशाही का शिकंजा इतना कस गया कि सैन्य नेतृत्व को नीति-निर्माण में आवाज़ तक नहीं दी जाती थी। हथियार ख़रीद में दलाली और कमीशन का दौर शुरू हुआ, जहाँ सैनिकों की ज़रूरत से ज़्यादा नेता और बिचौलियों की ज़रूरतें पूरी की जाती थीं। 1980 के दशक का बोफोर्स घोटाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना, जिसने न केवल भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता पर भी दाग लगाया। कांग्रेस ने उस घोटाले को ढँकने के लिए वही पुराना नैरेटिव अपनाया — “देश को तोड़ने वाली ताकतें सेना के नाम पर राजनीति कर रही हैं।” लेकिन असलियत यह थी कि सैनिक मर रहा था, और सत्ता के गलियारों में उसका खून सौदेबाज़ी का जरिया बन चुका था।
समय बदला, देश बदला, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता वही रही। 1999 के कारगिल युद्ध के समय जब भारतीय सेना ने असंभव को संभव कर दिखाया और दुश्मन को बर्फ़ीली चोटियों से खदेड़ दिया, तब भी कांग्रेस ने खुले मन से जयकार नहीं की। उस समय विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाए, मीडिया में संदेह के बीज बोए, और फिर वही पुरानी रट दोहराई — कि यह सब राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। यही वह क्षण था जब कांग्रेस ने प्रत्यक्ष रूप से सैनिक की वीरता पर संदेह जताकर यह संदेश दिया कि उसके लिए “राजनीतिक विरोध” राष्ट्रहित से बड़ा है।
यही सिलसिला 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी दिखा। जब दुनिया ने पहली बार भारत को निर्णायक प्रतिकार की मुद्रा में देखा, तो कांग्रेस नेताओं ने ही सबसे पहले उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। सैनिकों की बहादुरी पर अविश्वास जताकर उन्होंने शत्रु देशों के नैरेटिव को बल दिया। यह वही मानसिकता थी जो 1947 से कांग्रेस की आत्मा में बस चुकी थी — हथियार से नहीं, भाषण से जीतने की कोशिश करने वाली मानसिकता।
भारत का सैनिक जब सीमा पर दुश्मन से लड़ता है, तो उसके पीछे सिर्फ़ परिवार नहीं, पूरा देश खड़ा होता है। लेकिन कांग्रेस ने इस ‘राष्ट्रीय एकता’ के भाव को हमेशा संदेह और विभाजन के बीजों से कमजोर किया। उसे डर था कि अगर भारतीय समाज का केंद्र सैनिक बना, तो उसकी राजनीति का केंद्र ‘वंश’ नहीं रहेगा। इसलिए उसने सैनिक के स्थान पर नेता को, बलिदान के स्थान पर भाषण को, और तिरंगे के स्थान पर पार्टी के झंडे को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की।
सच्चाई यह है कि कांग्रेस का इतिहास भारत के सैनिकों के प्रति भय, ईर्ष्या और असुरक्षा का इतिहास रहा है। वह हमेशा उस भारत से डरती रही है जो आत्मविश्वासी हो, सशक्त हो, और अपने सम्मान के लिए लड़ सके। क्योंकि ऐसा भारत किसी “मातृसत्ता” या “वंशवादी” राजनीति की छाया में नहीं रहेगा। नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, कांग्रेस नेतृत्व का यही भय बार-बार झलकता रहा कि अगर जनता का भरोसा सेना और राष्ट्रभक्ति पर टिक गया, तो उसका विश्वास “परिवारवाद” की राजनीति से हट जाएगा।
लेकिन भारत का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही स्थायी उसका सैनिक का आत्मबल भी है। कांग्रेस ने सत्तर वर्षों तक सैनिकों के गौरव को मिटाने की कोशिश की, पर वह न मिटा सकी और न मिटा पाएगी। आज भी जब सीमा पर जवान ठंड में पहरा देता है, जब किसी वीर की अर्थी पर तिरंगा लहराता है, तो करोड़ों भारतीय उस भावना से एक हो जाते हैं जो किसी पार्टी नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। यही वह भावना है जो भारत को कांग्रेस की राजनीति से ऊपर उठाती है।
भारत के सैनिक ने कभी सत्ता नहीं मांगी, केवल सम्मान मांगा। यह वही सम्मान है जिसे कांग्रेस ने बार-बार छीनने की कोशिश की। लेकिन हर बार सैनिक ने अपने साहस से जवाब दिया — 1962 की हार के बाद 1965 की जीत से, 1971 के विभाजन के बाद 1999 के कारगिल से, और आज के बालाकोट से। इतिहास यह गवाही देता रहेगा कि जब-जब नेताओं ने देश को झुकाने की कोशिश की, तब-तब सैनिकों ने अपने रक्त से उसे सीधा खड़ा किया।
कांग्रेस का यह युद्ध भारत के सैनिकों के खिलाफ़ कभी बंद नहीं हुआ, यह सिर्फ़ बंदूकों से नहीं, शब्दों से, संस्थाओं से और वैचारिक ज़हर से लड़ा गया। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब भारतीय समाज कांग्रेस के इस “वैचारिक युद्ध” को पहचान चुका है। अब इतिहास वही नहीं रहेगा जो सत्ता लिखेगी — अब इतिहास वही होगा जो सैनिक ने अपने रक्त से लिखा है। और यही सच्चा भारत है — जो किसी परिवार के नाम पर नहीं, बल्कि अपने वीरों के नाम पर खड़ा है।