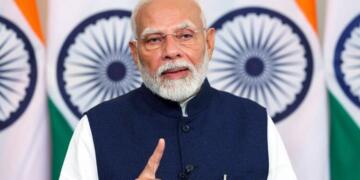1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि “न्यायपालिका में सुधार की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए। लगभग 800 जिला अदालतों के जजों के सामने राष्ट्रपति ने साफ कहा कि आम लोगों की नजर में अदालतें अब उनकी तकलीफ़ समझने में कमज़ोर पड़ती हैं। यानी लोगों को लगता है कि हमारी न्यायपालिका थोड़ी कठोर बन गई है।
राष्ट्रपति ने जजों की नियुक्ति प्रणाली पर सवाल उठया। उन्होंने कहा कि जिस तरह IAS अधिकारियों की नियुक्ति परीक्षा लेकर की जाती है उसी तरह जजों की नियुक्ति भी सख्त परीक्षा और जांच करने के बाद ही की जानी चाहिए।
पुराना मुद्दा: क्यों नहीं हुआ सुधार?
1958 में भारत के लो कमिशन ने ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस (AIJS) बनाने का प्रस्ताव दिया। बाद में 1978, 1986 और 2012 में भी यही सुझाव दोहराया गया। लेकिन हर बार खुद जजों ने इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का कहना रहा कि अगर ये व्यवस्था लागू हुई तो उनके अधिकार क्षेत्र में दखल होगा।
आज IAS, IPS और IRS जैसी बड़ी सेवाओं में चयन UPSC की परीक्षा से होता है। कानून की दुनिया में भी ICLS और ILS जैसी सेवाएँ हैं, मगर जज बनने की कोई सीधी व्यवस्था इनमें नहीं है।
कॉलेजियम प्रणाली: पारदर्शिता की कमी
कॉलेजियम सिस्टम में जजों की नियुक्ति का फैसला ज्यादातर जज ही करते हैं। आलोचकों का कहना है कि इसी वजह से इसमें रिश्तेदारी, जान-पहचान और पसंद-नापसंद का असर ज़्यादा दिखता है।
NJAC (नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन) इसी सिस्टम को सुधारने के लिए बनाया गया था। मोदी सरकार ने 2014 में 99वां संविधान संशोधन पास किया, 16 राज्यों ने मंजूरी दी और 2015 में कानून लागू हुआ। लेकिन अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को असंवैधानिक बता दिया और फिर से पुराना कॉलेजियम सिस्टम वापस ला दिया।
प्रधानमंत्री के सलाहकार संजीव सान्याल की चिंता
संजीव सान्याल, जो इतिहासकार और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, ने हाल ही में कानून विषयक सम्मेलन में तीन मुख्य बातें कही:
आज हमारी न्यायिक व्यवस्था खुद विकास में बड़ी रुकावट बनी हुई है। जब तक इसमें बड़े सुधार नहीं होंगे, तब तक मज़बूत आर्थिक नीतियाँ भी ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएँगी। इसी कड़ी में ‘माई लॉर्ड’ जैसी पुरानी शब्दावली पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग कहते हैं कि जज भी आम नागरिक ही हैं, कोई सामंती शासक नहीं। इसके अलावा अदालतों की लंबी छुट्टियाँ भी लोगों को खटकती हैं। जब बाक़ी सरकारी दफ्तर लगातार चलते रहते हैं तो फिर अदालतों का काम इतने दिनों तक क्यों ठप हो जाए?
बदलाव से क्या असर हो सकता है?
अगर नियुक्तियों में पारदर्शिता लाई जाए और IAS जैसी परीक्षा और ट्रेनिंग से जज चुने जाएँ तो ज़्यादा योग्य और सक्षम लोग न्यायपालिका में आएंगे। इससे केसों की निगरानी और फैसले तेज़ी से होंगे, और हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट तक मामले सालों तक अटके नहीं रहेंगे। आम लोगों के लिए भी न्याय पाना आसान होगा, अगर अदालतें साल भर सक्रिय रहें और लंबी छुट्टियाँ कम हों तो बैकलॉग भी घटेगा। साथ ही, मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से न्यायपालिका की रिपोर्टिंग और कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सलाहकार की टिप्पणियाँ साफ इशारा देती हैं कि न्यायपालिका में बड़े बदलाव की तैयारी है। इन सुधारों से तेज़ और सही न्याय मिलेगा, आर्थिक फैसलों में मदद होगी और न्यायपालिका आम आदमी के और करीब आएगी।