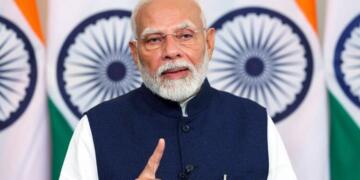सितंबर की एक सुबह दिल्ली के झंडेवालान कार्यालय में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सामने आए, तो मंच पर औपचारिकता कम और आत्मीयता ज्यादा थी। उन्होंने संघ की सौ वर्ष की यात्रा का जिक्र किया, लेकिन आंकड़ों और घोषणाओं से अधिक, उनके शब्दों में उन चेहरों की स्मृति थी जिन्होंने इस यात्रा को सम्भाला।
उन्होंने कहा संघ का कार्य केवल स्वयंसेवकों की शाखाओं से नहीं चलता। इस यात्रा के मूल में स्वयंसेवकों के परिवारों का सहयोग है। माताओं, बहनों और पत्नियों के त्याग से ही यह संभव हुआ कि कोई युवक प्रचारक बनकर देशभर में जाकर काम कर सका। होसबाले की यह स्वीकारोक्ति बताती है कि संघ की शताब्दी केवल संगठन की उपलब्धि नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की सामूहिक साधना का परिणाम है।
नागपुर से निकली चिंगारी
1925 का नागपुर, अंग्रेजों की सत्ता का दौर। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जिस समय संघ की नींव रखी, तब कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम की धुरी थी और क्रांतिकारी आंदोलन अपनी राह पर था। लेकिन हेडगेवार ने जिस काम की शुरुआत की, वह दीर्घकालिक था। उनके करीबी रहे अप्पाजी जोशी बाद में कहते थे हेडगेवार जी का विश्वास था कि भारत को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता से ही मजबूती मिलेगी।
हेडगेवार के साथियों में दादाराव परमार्थ, भाऊराव देवरस और यादवराव जोशी जैसे युवा थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई, नौकरी, परिवार तक छोड़ दिए। वे देशभर में शाखाओं के जरिए युवाओं को अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने लगे।
समाज की नब्ज पहचानना
संघ का सबसे बड़ा हथियार था उसका समाज से संवाद। न नारों का शोर और न ही सत्ता का प्रलोभन। बस रोज शाम को या सुबह में मैदान में लगने वाली शाखाएं। धीरे-धीरे इन शाखाओं ने गांव-गांव और मोहल्लों में जगह बना ली।
याद कीजिए विवेकानंद का वह कथन, जो होसबाले ने भी दोहराया था, चींटी को शक्कर खोजने के लिए अंग्रेज़ी नहीं चाहिए। भारत का समाज सात्विक कार्य को स्वयं ही पहचान लेता है। यही हुआ। ग्रामीण परिवारों ने बिना बड़े प्रचार-प्रसार के लिए स्वयंसेवकों को अपना लिया।
परिवार की मौन शक्ति
यह पहलू अक्सर छूट जाता है। प्रचारक के जीवन को देखकर लगता है मानो वह अकेला है, परिवार, गृहस्थी सब पीछे छोड़ चुका है। लेकिन यह आधा सच है। नागपुर की ही एक वृद्धा, जिनके पुत्र 1950 के दशक में संघ प्रचारक बने, ने एक बार कहा था, लोग कहते हैं मेरा बेटा घर छोड़ गया। मैं कहती हूं, वह तो घर को बड़ा कर गया। अब उसका घर पूरा भारत है।
इसी भाव ने संघ को मजबूती दी। माताएं अपने बेटों को विदा करती रहीं, पत्नियां अपने पतियों का साथ खोकर भी उनके निर्णय पर गर्व करती रहीं। बस यही त्याग संघ की शताब्दी यात्रा की रीढ़ है।
स्त्रियों का संगठित होना
1942 में जब मौसी जी लक्ष्मीबाई केलकर ने ‘राष्ट्र सेविका समिति’ बनाई, तो यह स्त्रियों के लिए समानांतर संगठन था। समिति ने न केवल महिलाओं को राष्ट्रसेवा से जोड़ा बल्कि उन्हें नेतृत्व की शिक्षा भी दी। बाद में प्रमिलाताई मेढ़े और अन्य सेविकाओं ने इसे अखिल भारतीय स्तर तक पहुंचाया। होसबाले जब शताब्दी वर्ष में मातृशक्ति के योगदान का स्मरण करते हैं, तो यह केवल औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि संगठनात्मक सत्य है, संघ की पूर्णता महिलाओं के सहयोग से ही संभव हुई।
विरोधियों का सहयोग : एक व्यापक विमर्श
संघ की यात्रा को समझना हो तो यह मानना पड़ेगा कि इसमें केवल अनुयायी ही नहीं, बल्कि समय-समय पर विरोधी भी सहभागी बने। 1981 में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में जब सैकड़ों हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ, तब संघ ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। मदुरै के पास आयोजित सम्मेलन में लगभग पांच लाख लोग जुटे। इस विशाल जनसभा की अध्यक्षता करने पहुंचे कांग्रेस नेता डॉ. कर्ण सिंह। विचारधारा के मतभेदों के बावजूद उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा को विभाजित नहीं होने देना चाहिए।
इसी तरह 1964 में जब विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ, तो मंच पर केवल संघ नहीं था। स्वामी चिन्मयानंद, मास्टर तारा सिंह, जैन मुनि सुशील कुमार और बौद्ध भिक्षु कुशोक बकुला भी थे। यह दिखाता है कि संघ का विमर्श संकीर्ण नहीं, बल्कि राष्ट्रीय था।
संतों का आशीर्वाद और सामाजिक क्रांति
संघ की विचारधारा का केंद्र हमेशा सांस्कृतिक पुनरुत्थान रहा है। श्री गुरुजी माधवा राव सदाशिव राव गोलवलकर ने 1960 में उडुपी में सम्मेलन बुलाया। विषय था अस्पृश्यता। सम्मेलन का उद्घोष बना-“हिंदवः सोदराः सर्वे” (सभी हिंदू आपस में भाई हैं)। यह उद्घोष उस दौर में एक सामाजिक क्रांति थी। ठीक उसी तरह जैसे प्रयाग सम्मेलन में कहा गया था-“न हिंदु पतितो भवेत्” (कोई हिंदू पतित नहीं हो सकता)। यही वह क्षण थे, जब संघ केवल संगठन नहीं रहा, बल्कि समाज सुधार की धारा बन गया।
प्रतिबंध और आपातकाल : परखा गया धैर्य
स्वतंत्रता के तुरंत बाद, 1948 में गांधी जी की हत्या के आरोप में संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। सरकार का इरादा इसे समाप्त करने का था। लेकिन कुछ ही महीनों में ही समाज का दबाव इतना बढ़ा कि प्रतिबंध हटाना पड़ा।
1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, तब संघ पर सबसे कठोर प्रहार हुए। हजारों स्वयंसेवक जेल में डाले गए। लेकिन जेल से बाहर वही कहानी दोहराई गई, परिवारों ने अपने बेटों, पतियों और भाइयों को त्यागा नहीं, बल्कि गर्व से संघ कार्य के लिए भेजा। प्राख्यात राजनीतिक विश्लेषक रामबहादुर राय कहते हैं, आपातकाल ने साबित किया कि संघ केवल शाखा में डंडा घुमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समाज की गहरी जड़ों से जुड़ा हुआ है।
समाज जीवन में शाखाएं
संघ का कार्य धीरे-धीरे समाज जीवन के हर क्षेत्र में फैल गया। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने मजदूरों को संगठित कर भारतीय मजदूर संघ खड़ा किया। दीनदयाल उपाध्याय ने राजनीति में ‘एकात्म मानववाद’ का दर्शन दिया। वनवासी कल्याण आश्रम ने आदिवासियों के बीच काम किया। सेवा भारती ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यानी शाखा का बीज, धीरे-धीरे विशाल वृक्ष बन गया जिसकी शाखाएं हर दिशा में फैलीं।
शताब्दी की नई चुनौती
आज संघ सौ वर्ष का होने जा रहा है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। समाज तेजी से बदल रहा है। गांव से शहर की ओर पलायन, तकनीक से पैदा हुआ नया जीवन और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की तीखी धार। इन सबके बीच होसबाले का शताब्दी वर्ष का संकल्प महत्वपूर्ण है—“घर-घर संपर्क।” यानी केवल शाखा में आने वाले युवाओं तक सीमित न रहकर हर घर तक राष्ट्रसेवा का संदेश पहुंचाना।
एक सदी की धड़कन
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा केवल संगठन की नहीं, बल्कि एक सभ्यता की धड़कन की यात्रा है। इसमें वह मां है, जिसने अपने बेटे को प्रचारक बनने के लिए भेजा, वह संत है जिसने समाज सुधार का आशीर्वाद दिया, वह राजनीतिक विरोधी है जिसने राष्ट्रीय प्रश्न पर साथ खड़ा होना स्वीकार किया। शताब्दी वर्ष इस गाथा का स्मरण है कि प्रतिबंधों, विरोध और उपहास के बावजूद संघ आज भी मजबूती से खड़ा है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
होसबाले के शब्दों में “संघ की शक्ति केवल शाखाओं की संख्या में नहीं, बल्कि उस समाज में है जिसने हमें बार-बार सहारा दिया।” सच यही है कि संघ की शताब्दी भारत की आत्मा की शताब्दी है।