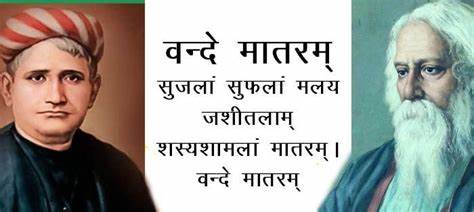भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि एक चेतना और राष्ट्र की आत्मा का उद्घोष रहा है। यह गीत बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की रचना ‘आनंदमठ’ का हिस्सा है, जिसे 1870 के दशक में लिखा गया। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और देश के अधिकांश हिस्सों में सामाजिक और राजनीतिक दबाव चरम पर थे। बंगाल, विशेषकर, अंग्रेजों की नीतियों के तहत आक्रोश और विद्रोह के केंद्र में था। ऐसे समय में बंकिमचंद्र ने जो गीत लिखा, उसमें केवल मातृभूमि की स्तुति नहीं थी, बल्कि यह भारतीय आत्मा और राष्ट्रवाद की आवाज़ भी थी।
वंदे मातरम् की पंक्तियां सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम, शस्यश्यामलां मातरम् के माध्यम से उन्होंने भारत की भूमि, जल और अन्न की महिमा को व्यक्त किया। यह गीत उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा बन गया। बंगाल विभाजन आंदोलन (1905) में इस गीत ने क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बुलंद किया। जेलों में बंद क्रांतिकारी इसे गाते हुए अपने बलिदान और त्याग के लिए प्रेरित होते थे। यह गीत, अपने भाव और ध्वनि से, औपनिवेशिक शक्ति के लिए चुनौती बन गया। ब्रिटिश अधिकारियों को यह समझ आ गया कि यह गीत केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की चेतना का प्रतीक है।
लेकिन, इतिहास में ऐसा देखने को मिलता है कि हर प्रतीक राजनीतिक दबावों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। 1937 में कोलकाता में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इसका एक प्रमाण है। यह बैठक 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चली, जिसमें पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाषचंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जेबी कृपलानी और अन्य प्रमुख नेता शामिल थे। उस समय मुस्लिम लीग लगातार यह प्रचार कर रही थी कि वंदे मातरम् हिंदू देवी दुर्गा की आराधना है और मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है। ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल नीति इस पर खेल रही थी।
कांग्रेस, उस समय के राजनीतिक दबाव से घबरा गई और एक समझौता किया गया। यह समझौता था कि वंदे मातरम् के केवल पहले दो छंदों को मान्यता दी जाए और बाकी भाग को हटा दिया जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि गीत की पूर्णता और उसकी सांस्कृतिक शक्ति आधी रह गई। यही वह क्षण था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में उजागर किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय वास्तव में राष्ट्र की आत्मा से दूरी का संकेत था और इसने भविष्य में विभाजन की मानसिकता को जन्म दिया।
टैगोर ने कभी नहीं किया वंदे मातरम का विरोध
रवींद्रनाथ टैगोर की भूमिका को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी ने उन्हें अपमानित किया। इतिहास बताता है कि टैगोर ने कभी भी वंदे मातरम् का विरोध नहीं किया। उन्होंने केवल यह कहा कि राजनीतिक मंच पर धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग सावधानीपूर्वक होना चाहिए ताकि सामाजिक और साम्प्रदायिक विवाद उत्पन्न न हो। टैगोर ने जन गण मन और वंदे मातरम् दोनों का सम्मान किया। मोदी का बयान टैगोर की आलोचना नहीं है, बल्कि कांग्रेस की उस मानसिकता पर प्रश्न है जिसने टैगोर के विचारों का केवल आंशिक उपयोग किया और राजनीतिक दबाव में राष्ट्रगीत की संपूर्णता को सीमित किया।
इस समय के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर राष्ट्र की चेतना को जीवित रखा। डॉ. हेडगेवार ने शाखाओं में वंदे मातरम् के नियमित गायन को राष्ट्रीय सेवा का हिस्सा बनाया। उनके लिए यह गीत केवल एक गान नहीं, बल्कि भारतमाता के प्रति समर्पण का प्रतीक था। गुरु गोलवलकर ने लिखा कि जो व्यक्ति वंदे मातरम् नहीं कह सकता, वह इस भूमि की आत्मा को नहीं समझ सकता। संघ की इस भूमिका ने उस समय की कांग्रेस की असहजता के विपरीत भारतीय संस्कृति को जीवित रखा।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यह विवाद समाप्त नहीं हुआ। संविधान सभा में बहस हुई कि राष्ट्रगान कौन सा होगा, जन गण मन या वंदे मातरम्? नेहरू चाहते थे कि राष्ट्रगान ऐसा हो जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी प्रयुक्त हो सके। राजेंद्र प्रसाद और अन्य कई सदस्य चाहते थे कि वंदे मातरम् को ही राष्ट्रगान बनाया जाए। अंततः समझौता हुआ—जन गण मन राष्ट्रगान और वंदे मातरम् राष्ट्रगीत। लेकिन कांग्रेस के भीतर वह असहजता बनी रही जो 1937 में उत्पन्न हुई थी।
प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान केवल औपचारिकता नहीं हैं। वे भारत की संस्कृति और राष्ट्र की आत्मा से जुड़े हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि 1937 का निर्णय विभाजन की मानसिकता की शुरुआत था। यह विभाजन केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि वैचारिक भी था। कांग्रेस ने उस समय अपने ही प्रतीकों से दूरी बनाई, जबकि आरएसएस और बाद में भाजपा ने उन प्रतीकों को जीवित रखा और उन्हें राष्ट्रीय एकता का आधार बनाया।
मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रवाद केवल आर्थिक या राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी समझा जाना चाहिए। आर्थिक विकास तभी स्थायी हो सकता है जब राष्ट्र अपनी आत्मा और प्रतीकों से जुड़ा हो। यही कारण है कि मोदी बार-बार “वंदे मातरम्” का पूरा महत्व और उसकी ऐतिहासिक पूर्णता पर जोर देते हैं।
आज भाजपा और आरएसएस वही सांस्कृतिक पुनर्जागरण आगे बढ़ा रहे हैं जिसे बंकिमचंद्र ने प्रारंभ किया। “वंदे मातरम्” के स्वर में वही ऊर्जा है जो भारत को औपनिवेशिक बंधनों से मुक्त कर सकती है और आधुनिक युग में आत्मविश्वास से भर सकती है। यह सिर्फ इतिहास की बहस नहीं, बल्कि आज की पीढ़ी के लिए भी चेतावनी और प्रेरणा का स्रोत है।
मोदी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का दृष्टिकोण आज भी वही पुरानी असहजता दर्शाता है। वह मानती है कि भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व न करे और प्रतीकों को विवाद का विषय बनाए। मोदी का राष्ट्रवाद इसका विरोध करता है और उसे पुनर्स्थापित करता है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत ने संविधान का निर्माण शुरू किया, तब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर तीव्र बहस हुई। यह बहस केवल संगीत या काव्य की नहीं थी, बल्कि राष्ट्र की आत्मा, उसकी सांस्कृतिक पहचान और उसकी भावनात्मक चेतना से जुड़ी थी। पंडित नेहरू और कुछ अन्य नेताओं का दृष्टिकोण था कि राष्ट्रगान ऐसा होना चाहिए जिसे वैश्विक मंच पर आसानी से स्वीकार किया जा सके, जिसकी धुन अंतरराष्ट्रीय रूप से तालमेल खा सके और जिसमें कोई समुदाय आहत न हो। इस विचारधारा के तहत उन्होंने जन गण मन का समर्थन किया।
लेकिन कई सदस्य, जिनमें राजेंद्र प्रसाद और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे, मानते थे कि वंदे मातरम् राष्ट्र की आत्मा का संपूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। उनके दृष्टिकोण में यह गीत केवल मातृभूमि की आराधना नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता, उसकी प्राकृतिक संपदा और उसके नागरिकों की एकता का प्रतीक था। अंततः समझौता हुआ कि जन गण मन राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम् राष्ट्रगीत। लेकिन यह समझौता कांग्रेस की असहजता को मिटा नहीं सका। वंदे मातरम् का सार्वजनिक गायन कई राज्यों में औपचारिक रोक या अनौपचारिक संकोच के कारण सीमित रह गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इस ऐतिहासिक असमानता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 1937 का निर्णय केवल गीत को आधा करने का नहीं था, बल्कि इससे राष्ट्र की आत्मा से दूरी बनाई गई। विभाजनकारी मानसिकता की जड़ें उसी समय पैदा हुईं। मोदी के दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं है; यह सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र की आत्मा से भी जुड़ा है। जब राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक पहचान और प्रतीकों से दूरी बनाता है, तब उसकी आत्मविश्वासपूर्ण प्रगति अस्थिर हो जाती है।
नेहरू और पटेल के बीच भी इस विषय पर मतभेद स्पष्ट था। नेहरू पश्चिमी उदारवाद और समाजवाद से प्रभावित थे और वे चाहते थे कि भारत की प्रतीकात्मक संस्कृति अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से शांत और उदार दिखे। पटेल, दूसरी ओर, भारतीय परंपरा और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के पक्षधर थे। उन्होंने बार-बार कहा कि भारत के प्रतीक केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का प्रतिबिंब हैं। इस मतभेद का प्रभाव कांग्रेस की नीति में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।
यहीं से भाजपा और आरएसएस की वैचारिक रेखाएं स्पष्ट हुईं। जनसंघ और बाद में भाजपा ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को राजनीति का केंद्र बनाया। उनके लिए वंदे मातरम् और भारत माता की जय केवल नारों या गीतों से अधिक थे। वे राष्ट्र की एकात्मता और भारतीयता का प्रतीक थे। मोदी इस परंपरा के आधुनिक उत्तराधिकारी हैं। उनका बयान कि 1937 में वंदे मातरम् के महत्वपूर्ण छंदों को हटा देना राष्ट्र की आत्मा से दूरी का संकेत था, उसी वैचारिक विरासत की पुष्टि करता है।
21वीं सदी में जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, तब अपने प्रतीकों पर गर्व का महत्व और बढ़ गया है। मोदी के नेतृत्व में वंदे मातरम् केवल गीत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, एकता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गया है। 2014 के लाल किले से भाषण, 2022 का हर घर तिरंगा अभियान, और राष्ट्रीय समारोहों में वंदे मातरम् का स्थान इस प्रतीकात्मक पुनर्परिभाषा को दर्शाते हैं।
मोदी के दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद केवल आर्थिक, राजनीतिक या सामरिक पहलुओं तक सीमित नहीं है। आर्थिक विकास तभी स्थायी हो सकता है जब नागरिक अपने देश के प्रतीकों, उसकी संस्कृति और उसकी ऐतिहासिक विरासत पर गर्व करें। यही कारण है कि मोदी बार-बार वंदे मातरम् के पूर्ण महत्व और उसकी ऐतिहासिक पूर्णता पर जोर देते हैं।
आज कांग्रेस का दृष्टिकोण वही पुराना संकोच दिखाता है। वह मानती है कि भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व न करे और प्रतीकों को विवाद का विषय बनाए। मोदी का राष्ट्रवाद इसका विरोध करता है और उसे पुनर्स्थापित करता है। यही वह अंतर है जो आज भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
वैश्विक स्तर पर भी वंदे मातरम् का महत्व बढ़ा है। भारतीय प्रवासी किसी भी मंच पर इसे गाते हैं, और यह केवल गीत नहीं, बल्कि भारतीयता की वैश्विक पहचान बन जाता है। यह भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे प्रामाणिक स्वर है, जो राजनीति नहीं, संस्कृति से उपजा है। मोदी का वक्तव्य केवल कांग्रेस को चुनौती नहीं देता; यह वैश्विक मंच पर भारत की अस्मिता का उद्घोष भी है।
विभाजन की मानसिकता और आज के भारत की स्थिति पर विचार करें। मोदी ने स्पष्ट किया कि 1937 का निर्णय राष्ट्र की विभाजनकारी सोच की शुरुआत था। यह केवल भौगोलिक विभाजन नहीं, बल्कि वैचारिक और मानसिक विभाजन था। कांग्रेस ने उस समय अपने ही प्रतीकों से दूरी बनाई, जबकि आरएसएस और बाद में भाजपा ने उन्हें जीवित रखा। आज मोदी उसी मानसिक विभाजन को पाट रहे हैं और भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुनर्स्थापित कर रहे हैं।
कांग्रेस की आलोचना कि मोदी को वर्तमान मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई और निवेश पर ध्यान देना चाहिए, केवल राजनीतिक असहमति है। मोदी का दृष्टिकोण व्यापक है। उनके लिए राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक चेतना आर्थिक विकास के लिए भी अनिवार्य हैं। आर्थिक नीति तभी स्थायी होगी जब राष्ट्र आत्मविश्वास और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा होगा।
वंदे मातरम् केवल गीत नहीं, बल्कि औपनिवेशिक बंधनों से मुक्ति, भारतीय आत्मा की पुनर्परिभाषा और आधुनिक भारत के लिए चेतना का स्रोत है। यह गीत इतिहास, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। मोदी का संदेश स्पष्ट है—भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करे, अपने प्रतीकों को संकोच के बिना अपनाए और राष्ट्र की पूर्ण चेतना में विश्वास करे।
इस बहस का सार यही है कि भारत की आत्मा जीवित रहे, उसकी सांस्कृतिक चेतना मजबूत हो और उसकी पहचान वैश्विक स्तर पर गर्व के साथ स्थापित हो। मोदी के दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नाम है। “वंदे मातरम्” इसके केंद्र में है।
अंततः, वंदे मातरम् की बहस केवल इतिहास या गीत की नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा, उसकी पहचान और उसके भविष्य की है। मोदी ने इसे स्पष्ट किया कि भारत तब तक पूर्ण राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक वह अपने प्रतीकों और गीतों पर गर्व नहीं करता। यही संदेश आज के भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
भारत का भविष्य तभी सुरक्षित और गर्वमय होगा जब हर नागरिक यह समझे कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और उसकी चेतना का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है। यह वही संदेश है जो मोदी बार-बार दोहरा रहे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना और राष्ट्र की आत्मा का पुनर्जागरण।