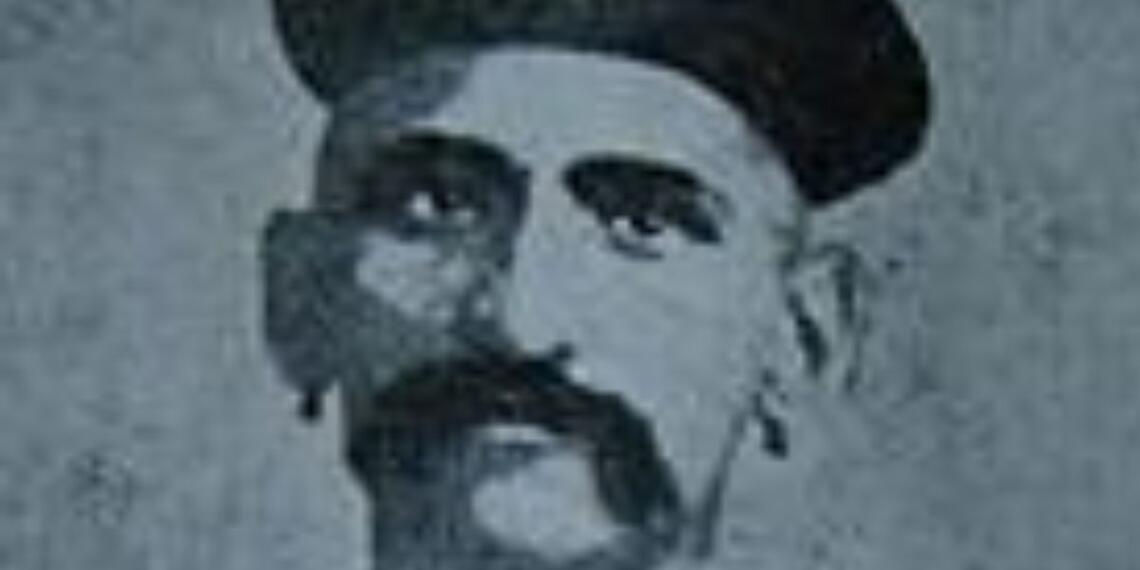आज, 18 अप्रैल को उस महान राष्ट्रभक्त दामोदर हरी चापेकर की पुण्यतिथि है जिस वीर ने विदेशी सत्ता की जड़ें हिलाने वाली पहली क्रांति की चिंगारी जलाई और जिसके सनातन समर्पण ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक नींव रखी। चापेकर बंधुओं में से एक दामोदर हरी चापेकर का जीवन केवल ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बल्कि यह राष्ट्र, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए उठाए गए आत्मबलिदान की गाथा थी। उनका पूरा परिवार राष्ट्रधर्म की वेदी पर समर्पित था तीनों भाइयों ने हंसते-हंसते फाँसी का फंदा स्वीकार किया, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं हुए। उनका संघर्ष राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं, बल्कि भारत की आत्मा उसकी सनातन संस्कृति और सामाजिक चेतना की रक्षा के लिए था। दामोदर हरी चापेकर ने जिस वातावरण में जन्म लिया, उसी में राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया।
आज उनकी पुण्यतिथि पर यह लेख उन विस्मृत क्रांतिकारियों को मुख्यधारा में लाने का एक प्रयास है, जिन्हें वामपंथी इतिहासकारों ने सुनियोजित तरीके से इतिहास से बाहर रखा। यह तिथि स्मरण कराती है कि भारत की स्वतंत्रता कोई राजनीतिक समझौता नहीं, बल्कि ऐसे बलिदानों की बुनियाद पर हासिल हुई थी, जिन्हें दशकों तक ऐतिहासिक विमर्श से दरकिनार किया गया।
तिलक थे प्रेरणा स्रोत
दामोदर हरि चापेकर उस वीर परिवार के अग्रज थे, जिन्होंने भारत माता की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका जन्म 25 जून, 1869 को पुणे में प्रसिद्ध कथावाचक श्री हरि विनायक पन्त के घर हुआ था। दामोदर के बाद उनके छोटे भाई बालकृष्ण (1873) और वासुदेव (1879) का जन्म हुआ। तीनों भाई बचपन से ही अपने पिता के साथ भजन-कीर्तन में भाग लेते थे, लेकिन उनका दिल मात्र धार्मिक कार्यों में नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा में भी लगा था।
तीनों भाई दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव इन वीर कथाओं को बचपन से ही सुनते-सुनते बड़े हुए। इन कहानियों ने उनके मन में परतंत्रता के खिलाफ आक्रोश और स्वराज्य के प्रति आत्मगौरव से भरी भावना को जन्म दिया। इन्हीं प्रेरणाओं के बीच दामोदर के हृदय में सैनिक बनने की प्रबल इच्छा जगी एक ऐसा सिपाही जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जीए और बलिदान दे।
दामोदर को गायन के साथ काव्यपाठ और व्यायाम का भी शौक था। उनके घर में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ‘केसरी’ नामक समाचार पत्र आता था, जिसे पूरे परिवार के साथ-साथ आस-पास के लोग भी पढ़ते थे। तिलक के विचारों से प्रेरित होकर, दामोदर ने युवकों का एक संगठन ‘व्यायाम मंडल’ तैयार किया और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति तिरस्कार की भावना को बढ़ावा दिया। जब तिलक जी को गिरफ्तार किया गया, तो दामोदर की आँखों में आँसू थे, परंतु उनकी माँ ने कहा, “तिलक जी ने हमें रोना नहीं, लड़ना सिखाया है।” यह बात दामोदर के दिल में बैठ गई, और उन्होंने जीवनभर उसी संघर्ष और समर्पण की राह पर चलने का संकल्प लिया।
इसके बाद दामोदर ने ‘राष्ट्र हितेच्छु मंडल’ के नाम से एक संगठन गठित किया, जिसमें युवकों को व्यायाम और शारीरिक सशक्तिकरण का प्रशिक्षण दिया जाता था। जब उन्हें वासुदेव बलवन्त फड़के की अमानवीय मृत्यु का समाचार मिला, तो दामोदर और उनके साथी सिंहगढ़ दुर्ग पर गए और वहाँ से यह संकल्प लिया कि वे फड़के के अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे।
यही नहीं राष्ट्रनिष्ठ परिवार की जड़ें वीरता और बलिदान से सिंचित थीं। इनके पूर्वजों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज्य स्थापना से लेकर बाजीराव पेशवा के अभियानों तक अनेक युद्धों में भाग लिया था और वीरगति को प्राप्त हुए थे। ऐसे बलिदानी पूर्वजों की गौरवगाथाएँ इस घर में बड़े गर्व से सुनाई जाती थीं। तीनों भाई दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव इन वीर कथाओं को बचपन से ही सुनते-सुनते बड़े हुए। इन कहानियों ने उनके मन में परतंत्रता के खिलाफ आक्रोश और स्वराज्य के प्रति आत्मगौरव से भरी भावना को जन्म दिया। इन्हीं प्रेरणाओं के बीच दामोदर के हृदय में सैनिक बनने की प्रबल इच्छा जगी। यही कारण था की आगे चलकर उन्होंने शस्त्र संचालन सीखने के लिए सेना में भर्ती होने का प्रयास किया पर उन्हें भर्ती नहीं किया गया। जिसके बाद उन्होएँ अपने पिता की तरह कीर्तन-प्रवचन करने लगे।
जब गुलामी की प्रतीक मूर्ति को पहनाई गई जूतों की माला
बात उन दिनों की है जब हरी चापेकर मुंबई पहुँचे थे। वहाँ एक सभा हो रही थी, रानी विक्टोरिया की मूर्ति के सामने जहाँ उसे देवी की तरह पूजने की कोशिश की जा रही थी। अंग्रेजों के अत्याचारों को सहते हुए भी जनता अगर गुलामी को सम्मान देने लगे, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता था? यही बात हरी चापेकर को भीतर तक झकझोर गई।
उन्होंने रातों-रात उस रानी विक्टोरिया की मूर्ति पर कालिख पोत दी और उसके गले में जूतों की माला लटका दी। ये कोई सामान्य विरोध नहीं था बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को दी गई खुली चेतावनी थी कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। इसी समय पुणे प्लेग की मार झेल रहा था। अंग्रेज सरकार ने ‘प्लेग कमिश्नर’ बनाकर मिस्टर रैण्ड को वहाँ तैनात किया। लेकिन बीमारी से ज्यादा डरावना बन गया उसका अमानवीय रवैया। रैण्ड अपने सिपाहियों के साथ हिंदुओं के घरों में बूट पहनकर घुसता, पूजाघरों को अपवित्र करता, और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता। ये सब अब ‘सरकारी कार्यवाही’ के नाम पर हो रहा था।
हरी चापेकर और उनके साथियों ने तय कर लिया अब चुप नहीं बैठना है। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक जवाब था। और जब उन्होंने अपने इस फैसले के बारे में लोकमान्य तिलक को बताया, तो तिलक ने सिर्फ समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि आशीर्वाद भी दिया।
मुस्कुराते हुए फाँसी के तख्ते पर झूल गए
सन 1897 में जब प्लेग की बीमारी ने भारत के कई हिस्सों में कहर बरपाना शुरू किया, पुणे भी उसकी चपेट में आ गया। बीमारी जितनी भयावह थी, उससे कहीं ज़्यादा निर्दयी था ब्रिटिश प्रशासन का रवैया। दो अंग्रेज अफसर वाल्टर चार्ल्स रैण्ड और आयर्स्ट को इस महामारी से निपटने के नाम पर पुणे भेजा गया, लेकिन इनका असली काम अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारों को संक्रमण से बचाने के बहाने आम जनता पर दमन करना था।
इनके आदेश से पुलिसकर्मी बूट पहने हुए हिंदू घरों में घुस जाते। पूजा स्थलों तक की पवित्रता को नहीं बख्शा जाता। लोग बीमार थे, डरे हुए थे, लेकिन शासन की क्रूरता ने उनकी पीड़ा को और बढ़ा दिया। ज़्यादा दुख की बात ये थी कि महिलाओं को भी अपमानित किया जाने लगा, रसोई और मंदिर तक सुरक्षित नहीं बचे थे। चापेकर बंधु दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव इन हालातों से भीतर तक विचलित हो चुके थे। वे देश और धर्म की मर्यादा को इस तरह कुचले जाते नहीं देख सकते थे। इन हालातों से कोई समाधान मिले, इस आस में वे लोकमान्य तिलक के पास पहुँचे। तिलक जी ने उन्हें शिवाजी महाराज का उदाहरण देते हुए कहा “अत्याचार के सामने झुकना कभी वीरों की परंपरा नहीं रही।” बस, यही एक बात थी जिसने तीनों भाइयों के मन में आग भर दी।
अब वे सिर्फ बोलने वाले नहीं थे, अब उन्होंने हथियार उठाने की ठान ली थी। उनका लक्ष्य साफ़ था अपने देशवासियों को इस अपमान से मुक्ति दिलानी है। 22 जून 1897 को पुणे के गवर्नमेंट हाउस में महारानी विक्टोरिया के शासन के साठ साल पूरे होने पर भव्य समारोह हो रहा था। रैण्ड और आयर्स्ट भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। उसी रात, दामोदर और बालकृष्ण अपने साथी विनायक रानडे के साथ वहां पहुँचे और इन अधिकारियों के लौटने का इंतज़ार करने लगे।
रात के क़रीब सवा बारह बजे, दोनों अंग्रेज अफसर अपनी-अपनी बग्घियों में सवार होकर निकले। जैसे ही रैण्ड की बग्घी आगे बढ़ी, दामोदर पीछे से चढ़ गए और गोली चला दी। उधर बालकृष्ण ने आयर्स्ट को निशाना बनाया। आयर्स्ट मौके पर ही मारा गया, जबकि रैण्ड ज़ख़्मी हो गया और कुछ दिन बाद अस्पताल में उसकी भी मौत हो गई।
इस साहसिक कार्रवाई की खबर पूरे शहर में फैल गई। जहाँ एक ओर पुणे की जनता ने चापेकर बंधुओं को हीरो की तरह देखा, वहीं अंग्रेज सरकार बौखला गई। बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू हुई। हर घर की तलाशी ली गई। चापेकर बंधुओं से जुड़े लोगों पर ज़ुल्म ढाया गया, लेकिन फिर भी वे पकड़ में नहीं आए। गुप्तचर विभाग के प्रमुख ब्रुइन ने ऐलान किया कि जो भी चापेकर बंधुओं के बारे में जानकारी देगा, उसे 20,000 रुपये इनाम मिलेगा। दुखद यह रहा कि उसी क्रांतिकारी संगठन में शामिल गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ नामक दो भाई लालच में आकर पुलिस से जा मिले और दामोदर का पता दे दिया।
इसके बाद दामोदर गिरफ्तार कर लिए गए। बालकृष्ण बच निकलने में सफल रहे। जब दामोदर को अदालत में पेश किया गया, तो उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ यह फैसला सुना जैसे कोई विजयी योद्धा अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहा हो। जेल में उनसे मिलने तिलक जी पहुँचे और उन्हें श्रीमद्भगवद्गीता भेंट की। 18 अप्रैल 1898, सुबह का समय। दामोदर हरि चापेकर हाथ में गीता लेकर शांति से फांसी के तख़्ते की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास था। उन्होंने मुस्कुराते हुए फांसी को गले लगाया।