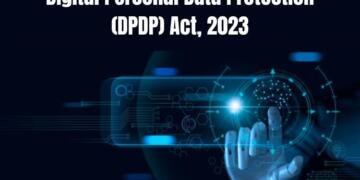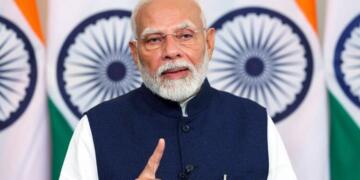एक फोटो इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। इसमें एक दुल्हन दो दूल्हों के साथ खड़ी है। ये दुल्हन है सुनीता चौहान, और उसने दो सगे भाइयों प्रदीप और कपिल नेगी से एक साथ शादी की है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के ट्रांस-गिरी इलाके के एक गांव की सच्ची घटना है। सुनीता की ये शादी कोई नई या अनोखी बात नहीं है। ये वहां की पुरानी जनजातीय परंपरा है, जिसे ‘जोड़ीदार प्रथा’ कहा जाता है। ये प्रथा हट्टी जनजाति में कई सालों से चली आ रही है, जिसमें एक ही महिला कई सगे भाइयों से शादी करती है।
प्राचीन सामाजिक संरचना का आधुनिक दृश्य
हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश के ट्रांस-गिरी क्षेत्र में रहने वाली एक पुरानी और परंपराओं से जुड़ी जनजातीय आबादी है। भारत सरकार ने इस जनजाति को वर्ष 2022 में अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe – ST) का दर्जा दिया। यह समुदाय कई पारंपरिक रिवाज़ों और सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। इन्हीं परंपराओं में से एक है भ्रातृ-पति बहुपति विवाह — जिसे अंग्रेज़ी में fraternal polyandry कहा जाता है। इस प्रथा के तहत एक महिला एक ही परिवार के कई सगे भाइयों से विवाह करती है और वे सभी उसके पति माने जाते हैं।
यह परंपरा केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी व्यावहारिक मानी जाती रही है। खासकर उन ग्रामीण इलाकों में जहां आजीविका का मुख्य आधार कृषि है। इतिहास में इस प्रथा का मकसद पारिवारिक ज़मीन का बंटवारा रोकना था ताकि खेतों का टुकड़ों में विभाजन न हो और परिवार की आर्थिक एकता बनी रहे। जब सभी भाई एक ही पत्नी से विवाह करते हैं, तो उनका घर संयुक्त रहता है और संसाधन बंटने की बजाय एक जगह केंद्रित रहते हैं।
समुदाय के बुजुर्गों का मानना है कि इस रिवाज़ से सिर्फ जमीन नहीं बचती, बल्कि परिवार का ढांचा भी मजबूत रहता है। महिला की देखभाल की जिम्मेदारी अकेले किसी एक व्यक्ति पर नहीं रहती, बल्कि सभी पति मिलकर उसे सहारा देते हैं। इससे महिलाओं की स्थिति को एक हद तक सुरक्षित माना जाता है, और बच्चों की परवरिश भी सामूहिक रूप से होती है।
सुनीता चौहान की हालिया शादी इस परंपरा का ताज़ा उदाहरण है। यह शादी पिछले छह वर्षों में समुदाय में हुई पाँचवीं बहुपति शादी है। यह दिखाता है कि भले ही समय बदला हो, लेकिन हट्टी जनजाति में यह परंपरा अब भी जीवित है और सामाजिक रूप से मान्य मानी जाती है।
भारतीय कानून और बहुपति विवाह: एक कानूनी ग्रे ज़ोन
भारतीय कानून में बहुपति और बहुपत्नी विवाह अपराध की श्रेणी में आते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता बहुविवाह को स्पष्ट रूप से अवैध मानते हैं। लेकिन इसमें एक कानूनी छूट भी है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार, जब तक केंद्र सरकार अधिसूचना जारी नहीं करती यह कानून अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता।
इसका मतलब यह है कि हट्टी जैसे जनजातीय समुदाय अपने परंपरागत और मौखिक रीति-रिवाज़ों के अनुसार विवाह कर सकते हैं, बशर्ते वे साबित कर सकें कि यह प्रथा लगातार चली आ रही है, तार्किक है, और सार्वजनिक नीति के खिलाफ नहीं है। अगर इस प्रथा को अदालत में चुनौती दी जाए, तो इसकी सच्चाई और वैधता साबित करने की जिम्मेदारी खुद समुदाय पर होती है, न कि सरकार पर।
UCC की पृष्ठभूमि में यह विवाह और भी अहम
जब भारत समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में सुनीता चौहान की दो भाइयों से शादी एक अहम कानूनी और सांस्कृतिक मिसाल बन गई है। 2024 में उत्तराखंड सरकार ने UCC लागू किया, जिसमें शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक जैसे नियम तय किए गए। इस कानून में बहुविवाह और बहुपति विवाह को साफ़ तौर पर प्रतिबंधित किया गया है और शादी का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
लेकिन, उत्तराखंड UCC नियमों की धारा 2 (2025) कहती है कि यह कानून अनुसूचित जनजातियों और संविधान के भाग XXI में संरक्षित रिवायती अधिकारों वाले समुदायों पर लागू नहीं होगा। यानी, एक तरफ जहां देश में UCC लागू करने की कोशिशें तेज़ हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ संविधान जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक स्वायत्तता और परंपराओं की रक्षा भी कर रहा है।
न्यायपालिका का दृष्टिकोण: परंपरा बनाम संविधान
भारतीय न्यायपालिका ने पिछले कुछ वर्षों में यह साफ़ कर दिया है कि कोई भी परंपरा तभी तक मान्य मानी जा सकती है, जब तक वह संविधान के मूल सिद्धांतों जैसे समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के खिलाफ न हो। यानी यदि कोई रिवाज़ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे केवल ‘परंपरा’ कहकर सही नहीं ठहराया जा सकता।
2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया, यह मानते हुए कि एकतरफ़ा त्वरित तलाक की यह प्रथा महिलाओं के साथ अन्याय करती है और उनके समानता (अनुच्छेद 14) और गरिमा व जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करती है।
2018 में सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी धार्मिक परंपरा को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह लैंगिक भेदभाव करती है।
- जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ‘रामचरण बनाम सुखराम’ मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया कि अगर किसी जनजातीय परंपरा में महिलाओं को संपत्ति का हक़ नहीं मिलता या उस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें हक़ से वंचित किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि परंपराएं भी समय के साथ बदलनी चाहिए और उन्हें संविधान के अधिकारों से ऊपर नहीं रखा जा सकता।
सवाल जो इस शादी से उठते हैं
सुनीता की शादी सिर्फ एक अद्वितीय सांस्कृतिक घटना नहीं, बल्कि एक संवैधानिक बहस भी है। क्या जनजातीय समुदायों को परंपरा के नाम पर अलग कानूनी छूट मिलनी चाहिए? क्या यह छूट महिला अधिकारों और समानता के सिद्धांतों से टकराती है? क्या समान नागरिक संहिता का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब वह सभी समुदायों पर समान रूप से लागू हो?
भारत का संविधान संस्कृति और विविधता का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी परंपरा मौलिक अधिकारों के खिलाफ न जाए। सुनीता चौहान की शादी ने इन दोनों के बीच खींची गई रेखा को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। यह शादी एक तरफ हट्टी समुदाय की पहचान और सामाजिक संरचना को दर्शाती है, और दूसरी ओर यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में कानून, परंपरा और अधिकारों की जटिलता को उजागर करती है।
जब भारत UCC की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे विवाह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनते जा रहे हैं। क्या हमें परंपराओं को उसी रूप में चलने देना चाहिए, या उन्हें आधुनिक भारत के संविधान की कसौटी पर कसना चाहिए? इस सवाल का उत्तर शायद आने वाले वर्षों में देश की कानूनी, सांस्कृतिक और राजनीतिक दिशा तय करेगा।