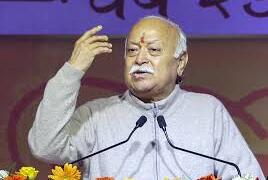मुजफ्फरपुर, उत्तर बिहार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। व्यापार, शिक्षा और राजनीति का यह गढ़ लंबे समय से अपराधियों के लिए भी सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा। 90 के दशक में यहाँ कई आपराधिक गिरोह सक्रिय थे, जो अपहरण और फिरौती से अपना साम्राज्य खड़ा कर चुके थे।
बिहार में “जंगलराज” शब्द महज एक राजनीतिक जुमला नहीं था, बल्कि 1990 से 2005 के बीच आम आदमी की रोज़मर्रा की हकीकत थी। यह वह दौर था जब अपराध और सत्ता का गठजोड़ इतना मजबूत हो चुका था कि कानून-व्यवस्था केवल कागज़ पर ही मौजूद थी। अपहरण, फिरौती और हत्या जैसे अपराध संगठित धंधे में बदल चुके थे। ट्रेन से लेकर सड़क और गांव से लेकर शहर तक, हर जगह असुरक्षा का आलम था। इसी अंधकारमय पृष्ठभूमि में मुजफ्फरपुर का गोलू हत्याकांड घटित हुआ, जिसने न केवल शहर बल्कि पूरे बिहार को हिला दिया।
मुजफ्फरपुर, उत्तर बिहार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। व्यापार, शिक्षा और राजनीति का यह गढ़ लंबे समय से अपराधियों के लिए भी सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा। 90 के दशक में यहाँ कई आपराधिक गिरोह सक्रिय थे, जो अपहरण और फिरौती से अपना साम्राज्य खड़ा कर चुके थे। डॉक्टर, व्यापारी, इंजीनियर और संपन्न परिवार उनके लिए सोने की खान थे। ऐसे ही दौर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार का मासूम बच्चा गोलू अपराधियों का शिकार बना।
गोलू का अपहरण दिनदहाड़े हुआ। परिवार को फोन आया कि भारी रकम चुकाओ, तभी बच्चा वापस मिलेगा। यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उस समय अपहरण बिहार में लगभग रोज़ का किस्सा था। लेकिन गोलू का परिवार उम्मीद लगाए बैठा था कि पुलिस और प्रशासन मदद करेगा। उन्होंने गुहार लगाई, थानों के चक्कर काटे, लेकिन कार्रवाई ढीली और लचर रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे परिवार से सीधे बातचीत करते रहे। दिनों तक इंतज़ार के बाद अचानक खबर आई कि गोलू की हत्या कर दी गई है।
इस मासूम की लाश मिलते ही पूरे मुजफ्फरपुर में मातम और गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर निकल आए, दुकाने बंद हो गईं और जगह-जगह टायर जलाकर प्रदर्शन शुरू हो गए। भीड़ ने साफ़-साफ़ कहा—“अगर पुलिस समय रहते कुछ करती तो बच्चा जिंदा होता।” यह आक्रोश महज़ एक हत्या के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ था जो अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुका था।
जनता का गुस्सा इतना उग्र था कि हालात बेकाबू हो गए। नारेबाज़ी, पथराव और तोड़फोड़ के बीच प्रशासन पूरी तरह बेबस दिखाई देने लगा। इस उग्र माहौल में सबसे नाटकीय घटना उस समय के मुजफ्फरपुर एसपी नैयर हसनैन खान से जुड़ी थी। भीड़ का निशाना सीधे उन पर था। गुस्साए लोगों ने पुलिस अधिकारियों को घेर लिया और हालात इतने बिगड़े कि प्रशासन को खुद की सुरक्षा के लिए एसपी साहब को ही थाने के हाजत (लॉकअप) में बंद करना पड़ा।
पूरा दिन वे वहीं बंद रहे। यह नज़ारा इतना अविश्वसनीय था कि जिसने भी देखा, दंग रह गया। आमतौर पर अपराधियों को हाजत में डाला जाता है, लेकिन यहाँ जिले के पुलिस प्रमुख को जनता के गुस्से से बचाने के लिए उसी हाजत में कैद कर दिया गया। यह तस्वीर बिहार की कानून-व्यवस्था की सबसे भयावह और शर्मनाक मिसाल बन गई। उस दिन मानो पूरा मुजफ्फरपुर यह कह रहा था—“पुलिस हमें नहीं बचा सकती, पुलिस खुद को भी नहीं बचा पा रही है।”
गोलू हत्याकांड केवल एक बच्चे की हत्या नहीं था, यह उस दौर की राजनीति और प्रशासनिक नाकामी का आईना था। अपहरण उस समय संगठित उद्योग बन चुका था। हर गैंग का अपना नेटवर्क, अपना इलाका और अपने राजनीतिक संरक्षक थे। अपहरण की रकम से न केवल अपराधियों की जेबें भरती थीं, बल्कि चुनावों में उसका इस्तेमाल भी होता था। पीड़ित परिवार पुलिस पर भरोसा नहीं करते थे, वे चुपचाप फिरौती चुका कर मामले को रफा-दफा करने में ही समझदारी मानते थे। गोलू का परिवार भी असहाय था, लेकिन अपराधियों ने पैसे की परवाह किए बिना मासूम को मौत के घाट उतार दिया। यही इस केस को और भयावह और प्रतीकात्मक बना देता है।
घटना के बाद मीडिया ने इस कांड को व्यापक रूप से उठाया। अख़बारों की सुर्ख़ियों में यही खबर छाई रही। पत्रकारों ने इसे “जंगलराज की पराकाष्ठा” बताया। प्रभात खबर समेत कई स्थानीय अखबारों ने विस्तार से लिखा कि कैसे एक बच्चे की हत्या ने पूरे शहर को सन्न कर दिया और किस तरह एसपी तक को हाजत में छिपना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर भी यह घटना जंगलराज की गूंज लेकर पहुँची। विपक्षी दलों ने इसे सत्ता पर हमला करने का हथियार बना लिया। चुनावी सभाओं में “जंगलराज” शब्द पहले से ज़्यादा ताक़त के साथ गूंजने लगा।
इस कांड के सामाजिक असर दूरगामी रहे। व्यापारी परिवारों ने अपने बच्चों को बाहर भेजना शुरू कर दिया। कई परिवार स्थायी रूप से दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में बस गए। जिनका कारोबार यहीं रहा, उन्होंने भी जीवन जीने का तरीका बदल लिया—शाम ढलते ही लोग घरों में बंद हो जाते थे और किसी भी अनजान व्यक्ति को शक की निगाह से देखते थे।
गोलू हत्याकांड ने यह साफ़ कर दिया कि प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह चरमरा चुका है। एफआईआर दर्ज करने से लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी तक, हर कदम पर लापरवाही और दबाव झलकता रहा। जनता का भरोसा टूट चुका था। यही वजह थी कि लोग सीधे शासन के खिलाफ उतर आए।
यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी समाज में न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक निष्पक्षता कितनी आवश्यक है। जब राजनीति अपराधियों को संरक्षण देती है और पुलिस-प्रशासन जनता की सुरक्षा के बजाय अपराधियों से डरने लगता है, तब हालात ऐसे ही बनते हैं। गोलू हत्याकांड ने यह साबित कर दिया कि जंगलराज केवल एक राजनीतिक मुहावरा नहीं था, बल्कि जनता की रोज़मर्रा की हकीकत थी।
आज भी जब लोग जंगलराज की चर्चा करते हैं, तो गोलू हत्याकांड जैसे उदाहरण सबसे पहले याद आते हैं। यह न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि पूरे बिहार के लिए शर्मनाक और दर्दनाक स्मृति है। सवाल आज भी गूंजता है—अगर पुलिस और प्रशासन सजग होता, अगर राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर काम होता, तो क्या गोलू ज़िंदा होता?
गोलू की हत्या केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं थी। यह पूरे समाज की पीड़ा थी। वह मासूम बच्चा उस दौर की भयावहता का प्रतीक बन गया, जब आम आदमी अपने बच्चों को खेलते देख भी डरता था कि कहीं अगला शिकार वही न हो जाए।