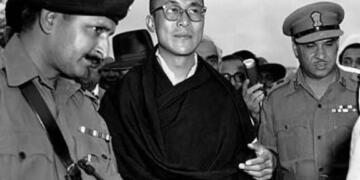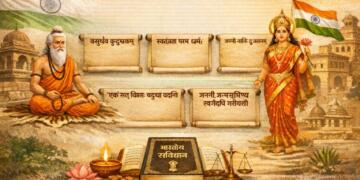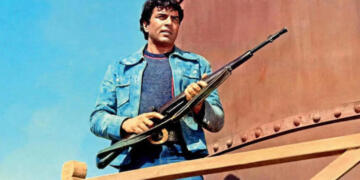काठमांडू की गलियों में जलते टायरों का धुआं अभी तक छंटा नहीं है। संसद भवन की टूटी खिड़कियां और सर्वोच्च न्यायालय के बाहर गुस्साई भीड़ इस बात का सबूत हैं कि नेपाल का लोकतंत्र गहरी दरारों में फंस चुका है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफ़ा देना पड़ा, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल तक सुरक्षित ठिकाने पर चले गए। द काठमांडू पोस्ट ने लिखा—“यह केवल सत्ता का संकट नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का ढहना है।”
नेपाल में यह विस्फोट अचानक नहीं हुआ। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और नेताओं का चीन की ओर झुकाव धीरे-धीरे जनता की सहनशक्ति को खत्म कर रहा था। लेकिन जब सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, तो आग में घी पड़ गया। बीबीसी नेपाली सेवा की रिपोर्ट कहती है—“डिजिटल पीढ़ी को चुप कराना, उस भूचाल का पहला झटका था जिसने सत्ता को हिला दिया।”
2006 में नेपाल ने खुद को हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया था। उस समय इसे ऐतिहासिक कदम बताया गया। लेकिन आज आंदोलन में शामिल बहुत से युवा खुलकर कह रहे हैं कि उनकी सांस्कृतिक पहचान उनसे छीनी गई। हिमालयन टाइम्स की एक टिप्पणी के अनुसार, “नेपाल का धर्मनिरपेक्ष मॉडल जनता के बड़े हिस्से को कभी स्वीकार्य नहीं हुआ। यह असंतोष अब सड़क पर दिखाई दे रहा है।”
इसके साथ ही नेपाल ने विदेश नीति में भी भारी भूल की। भारत जैसे स्वाभाविक साझेदार से दूरी बनाकर चीन से करीबी बढ़ाई। बीजिंग ने अरबों डॉलर के निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का वादा किया। काठमांडू को लगा कि यही विकास का रास्ता है। लेकिन द डिप्लोमैट पत्रिका का विश्लेषण बताता है कि “ज्यादातर चीनी परियोजनाएँ भ्रष्टाचार और देरी की भेंट चढ़ गईं। जनता को न रोज़गार मिला, न राहत।”
भारत से दूरी बनाने की यह रणनीति आत्मघाती साबित हुई। इंडियन एक्सप्रेस ने हाल में लिखा—“नेपाल भूल गया कि उसका रिश्ता दिल्ली से सिर्फ कूटनीति का नहीं, बल्कि संस्कृति और आस्था का है। रोटी-बेटी का रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता।” जब ओली सरकार ने नक्शे का विवाद छेड़ा और सीमा पर तनाव बढ़ाया, तो उसने भारत को नाराज़ करने के साथ अपने ही समाज को और उलझा दिया।
आज आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा नेपाल का युवा है। सोशल मीडिया पर सक्रिय यह पीढ़ी भ्रष्टाचार और चीन-परस्ती दोनों के खिलाफ खड़ी है। 22 वर्षीय छात्रा अनुष्का श्रेष्ठ ने एक स्थानीय चैनल से कहा—“हम लोकतंत्र इसलिए नहीं चाहते कि नेता चीन की कठपुतली बनें। हमें पारदर्शिता और पहचान चाहिए।” यही आवाज़ आज पूरे नेपाल में गूंज रही है।
भारत के लिए यह केवल पड़ोसी का संकट नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। अगर नेपाल अस्थिर रहता है, तो यह माओवादी और आतंकी संगठनों के लिए उर्वर ज़मीन बनेगा। द हिन्दू की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत-नेपाल सीमा पर पहले से अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी पड़ी है। दिल्ली की चिंता साफ है—बीजिंग इस अस्थिरता का फायदा उठाकर हिमालय के रास्ते भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है।
नेपाल का यह संकट पूरे दक्षिण एशिया के लिए चेतावनी है। लोकतंत्र केवल संवैधानिक ढांचे से नहीं चलता, बल्कि जनता के भरोसे से जिंदा रहता है। जब संसद और न्यायपालिका पर भीड़ हमला करती है, तो संदेश साफ होता है कि जनता की आस्था पूरी तरह टूट चुकी है।
भारत के लिए भी यह सीख है कि उसे नेपाल को अपने पाले में रखने के लिए सिर्फ कूटनीतिक भाषा काफी नहीं। सांस्कृतिक रिश्तों, धार्मिक धरोहरों और रोज़गार के अवसरों के ज़रिए जनता के दिल में जगह बनाना ज़रूरी है। यही वह रास्ता है जो नेपाल को फिर से स्थिर कर सकता है और भारत की सुरक्षा को मज़बूत कर सकता है।
काठमांडू की सड़कों पर उठते धुएँ के बीच सवाल गूंज रहा है—क्या नेपाल हिंसा और अराजकता में और डूबेगा, या इस संकट को अवसर बनाकर अपने लोकतंत्र और पहचान को फिर से गढ़ेगा? और सबसे अहम, क्या वह समझ पाएगा कि भारत से दूरी और चीन से करीबी उसकी सबसे बड़ी भूल रही है?