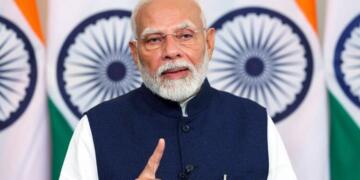भारत की हर परंपरा की जड़ में कोई गहरी कथा होती है। कहीं विश्वास, कहीं भय, कहीं प्रेम और कहीं उन तीनों का सम्मिश्रण। भाई दूज, जो अधिकांश भारत में रक्षाबंधन की तरह भाई-बहन के स्नेह का पर्व है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में एक अद्भुत और गहन मनोवैज्ञानिक रूप ले लेता है। यहां बहनें पहले अपने भाई को मरने का श्राप देती हैं और फिर जीभ में कांटा चुभाकर उस श्राप को स्वयं निष्प्रभावी करने की प्रक्रिया से गुजरती हैं। यह अनुष्ठान जितना विचित्र लगता है, उतना ही गहरा अर्थ अपने भीतर समेटे हुए है, जहां प्रेम अपराधबोध से टकराता है, और स्नेह त्याग में बदल जाता है।
श्राप देने की परंपरा: प्रेम का कठोर रूप
इस परंपरा का आरंभ किसी प्राचीन मिथक से जुड़ा बताया जाता है, जो लोक कथाओं में अब भी जीवित है। कथा कहती है कि एक समय बहन ने अपने भाई को क्रोध में आकर श्राप दे दिया थाकि उसका जीवन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से प्रार्थना की कि भाई की आयु बची रहे और अपनी जीभ में कांटा चुभाकर यह प्रण लिया कि आगे से वह हर भाई दूज पर वही कष्ट सहकर अपने भाई के जीवन का प्रायश्चित करेगी। धीरे-धीरे यह कथा लोक में जीवंत होती गई, और आज यह एक अद्भुत रीत के रूप में जीवित है।
श्राप यहां घृणा या द्वेष का प्रतीक नहीं, बल्कि भावनाओं के विस्फोट का है। जैसे कोई मां बच्चे को डांटकर रो पड़ती है, वैसे ही बहन यहां भाई को मृत्यु का श्राप देकर उसी क्षण उसके जीवन के लिए खुद को पीड़ा देती है। यह परंपरा इस बात की प्रतीक है कि रिश्तों में प्रेम हमेशा ‘मधुर’ रूप में ही नहीं जीया जाता, कभी-कभी प्रेम के साथ अपराधबोध, भय और त्याग भी जुड़ा होता है।
जीभ में कांटा क्यों?
कांटा यहां आत्मसंयम और पीड़ा का प्रतीक है। जब बहन अपनी जीभ में कांटा चुभाती है, तो यह न केवल अपने वचन के प्रभाव को निष्क्रिय करने का प्रतीक है, बल्कि यह एक तरह का ‘व्रत’ भी है। एक शारीरिक कष्ट, जो आत्मिक प्रायश्चित को मूर्त रूप देता है।
यह परंपरा यह भी दर्शाती है कि भारतीय लोक में स्त्री हमेशा ही त्याग और तपस्या का केंद्र रही है। जब कोई बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए खुद को दर्द देती है, तो यह उस मातृत्व भाव की झलक भी है जो भारतीय नारी के हर रूप में झलकता है। वह न सिर्फ जीवन देती है, बल्कि उसकी रक्षा के लिए खुद को कष्ट में भी डालती है।
अंधविश्वास या मनोविज्ञान?
आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो यह परंपरा अंधविश्वास प्रतीत होती है। परंतु सामाजिक और मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह एक रिचुअल ऑफ गिल्ट एंड रिपेंटेंस (अपराधबोध और प्रायश्चित की रस्म) है। भाई-बहन का रिश्ता भारतीय समाज में हमेशा ही भावनाओं की चरम सीमा पर रहा है। संरक्षण, प्रेम, गुस्सा, स्वामित्व और त्याग सब कुछ उसमें घुला हुआ है। इस परंपरा में बहन का श्राप और फिर आत्मदंड, इन दो चरम अवस्थाओं का मिलन है। वह पहले उस भय को साकार करती है कि अगर भाई मर जाए तो? और फिर उस भय को परास्त करने के लिए खुद को कष्ट देती है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से ‘कांटे का चुभना’ उस भाव का प्रतीक है, जिसमें बहन अपने डर, अपने अपराधबोध और अपने स्नेह को एक साथ स्वीकार करती है।
स्थानीय भिन्नताएं और धार्मिक स्वर
बिहार के कुछ जिलों जैसे सीवान, गोपालगंज, और भोजपुर में इस परंपरा को भौजी-दूज या कांटा-दूज कहा जाता है। वहीं झारखंड के पलामू और गढ़वा इलाकों में इसे काटी-दूज कहा जाता है। कई जगहों पर यह कांटा असली नहीं होता, बल्कि ‘तुलसी की लकड़ी’ से बना छोटा प्रतीकात्मक कांटा होता है, जिसे बहन जीभ पर स्पर्श कर ‘पाप-प्रायश्चित’ करती है। हालांकि, अधिकांश जगहों पर रेगनी (एक प्रकार की घास) का कांटा चुभाया जाता है।
छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में इसे बइना दूज कहा जाता है, जहां बहन भाई को पहले प्रतीकात्मक रूप से श्राप देती है और फिर खुद का व्रत खोलने से पहले कांटे का स्पर्श करती है। कुछ इलाकों में इस दिन बहनें उपवास भी रखती हैं, और कांटा चुभाने से पहले मिट्टी की ‘गौरी’ मूर्ति से प्रार्थना करती हैं कि भैया के जीवन का हर संकट मेरे दर्द में समा जाए।
लोकगीतों में दर्द और प्रेम का संगम
इस रीत से जुड़े लोकगीत अत्यंत करुण और भावनात्मक हैं। उनमें एक बहन अपने भाई से कहती है—
“भैया, मउसी के आंगन जइबू, मोर कइसे रहबू तोरा बिन,
श्राप देतानी, फिर कांटा चुभाईं, मोर दुख से बाँचबू तू जिन।”
(भैया, जब तू मउसी के घर जाएगा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? मैं तुझे श्राप देती हूं, पर फिर कांटा चुभाकर तेरा जीवन अपने दुख में खरीद लूंगी।) यहां श्राप प्रेम का छद्म है। वह प्रेम जो अत्यधिक है, जो इतना प्रबल है कि वह त्याग में बदल जाता है।
सांस्कृतिक प्रतीक और सामाजिक अर्थ
यह परंपरा सिर्फ एक धार्मिक रीत नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतीक भी है। यह हमें बताती है कि भारतीय संस्कृति में हर भावना को एक अनुष्ठान में बदल दिया गया। गुस्सा हो या प्रेम, अपराधबोध हो या त्याग-हर चीज को एक प्रतीक मिला दिया जाता है।
इस रीत में स्त्री की भूमिका उस संयमित ऊर्जा की है, जो अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेती है। जब वह श्राप देती है, तो अपनी वाणी के दुष्परिणाम से डरती है और उसी क्षण उसे निष्क्रिय करने के लिए आत्मत्याग करती है। यह भारतीय संस्कृति की उस गहरी समझ का हिस्सा है, जिसमें वचन और व्रत दोनों की समान प्रतिष्ठा है।
समाज में बदलती धारणा
आज के शहरी समाज में यह परंपरा तेजी से लुप्त हो रही है। आधुनिक पीढ़ी इसे पुराना अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज करती है। लेकिन गांवों में आज भी महिलाएं इसे अपने जीवन की आस्था मानती हैं। उनके लिए यह कांटा चुभाना दर्द नहीं, बल्कि प्रेम का चरम रूप है। एक ऐसी अनुभूति, जो रिश्ते को शब्दों से ऊपर उठाकर कर्म में बदल देती है।
समाजशास्त्रियों का कहना है कि यह परंपरा भारत के ग्रामीण समाज में महिला की भावनात्मक जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। वह केवल प्रेम जताने तक सीमित नहीं, बल्कि अपने रिश्ते के हर परिणाम की जवाबदेही भी लेती है। चाहे वह शब्दों का पाप हो या भावनाओं का तूफान।
प्रेम का दार्शनिक अर्थ: कांटा जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं
दर्शन के स्तर पर देखें तो यह परंपरा हमें सिखाती है कि हर प्रेम में एक कांटा होता है, जो चुभता भी है और जोड़ता भी। अगर वह न हो, तो प्रेम में गहराई नहीं रहती। इसीलिए भारतीय लोकजीवन में कांटा ‘पीड़ा’ का प्रतीक नहीं, बल्कि ‘अनुभूति’ का प्रतीक है।
भाई दूज की यह परंपरा यही कहती है कि प्रेम को बचाने के लिए कभी-कभी हमें उसे दर्द में तपाना पड़ता है। बहन का कांटा उस अग्नि की ही तरह है, जो रिश्ते को पवित्र और स्थायी बनाता है।
आधुनिकता की चमक में जब सबकुछ आसान और सतही होता जा रहा है, तब इस तरह की परंपराएं हमें आज भी याद दिलाती हैं कि भारतीय समाज ने प्रेम को कभी सस्ता नहीं समझा। यहां हर रिश्ते की कीमत है, हर शब्द का अर्थ है और हर भावना का अपना दायित्व।
बिहार-झारखंड की यह भाई-दूज हमें सिखाती है कि प्रेम केवल फूल नहीं है, उसमें कांटे भी हैं, लेकिन वही कांटे रिश्तों को असली गहराई देते हैं। बहन का यह अनोखा अनुष्ठान एक भावनात्मक दर्शन है, जहां श्राप, वरदान में बदल जाता है और पीड़ा, प्रार्थना में।