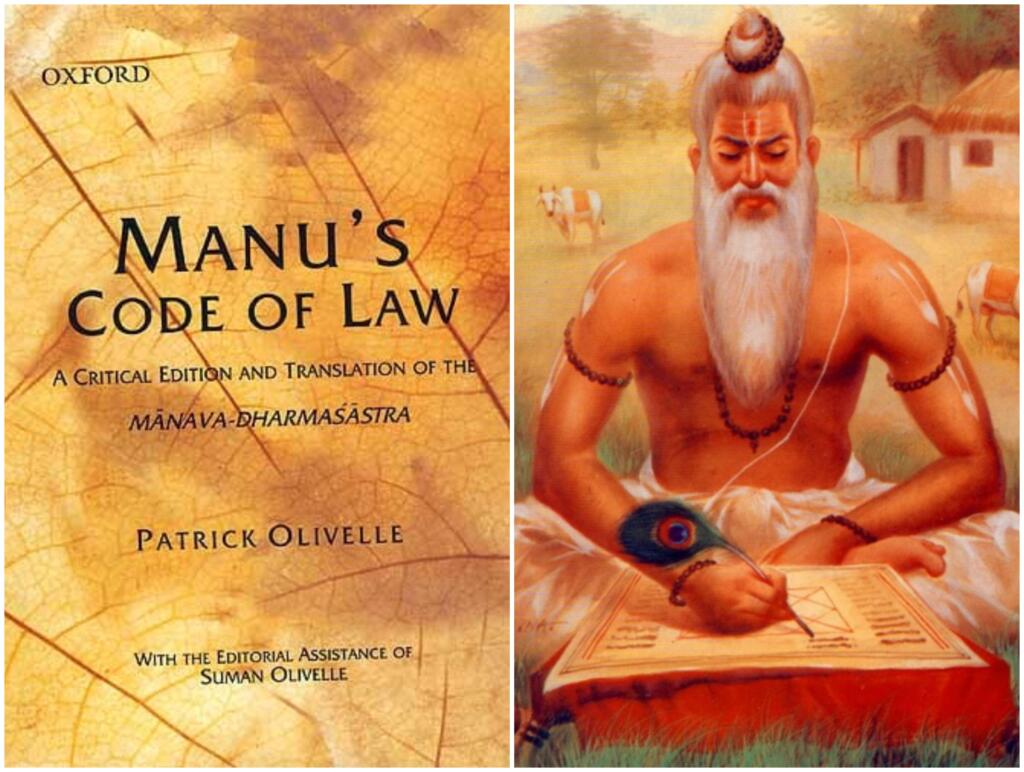मनु ने न्याय और समानता (justice and equity) की अवधारणाओं पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि जो भी व्यक्ति न्याय का उल्लंघन करता है, वह सदैव घृणास्पद होता है। राजा मूल न्यायालय (original court) और अपील न्यायाधिकरण (appellate tribunal) — दोनों की भूमिका निभाता है और न्याय का संचालन करता है। वह स्वयं न्यायपालिका का प्रधान होता है और इसमें उसका सहयोग ब्राह्मणों और अनुभवी सभासदों द्वारा किया जाता है। न्याय का निर्धारण धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों और स्थानीय परंपराओं (regional customs) के अनुसार होना चाहिए।
यदि किसी कारणवश राजा स्वयं न्याय नहीं कर पाता, तो वह एक विद्वान ब्राह्मण तथा तीन सभ्यों (सहायक न्यायाधीशों) को नियुक्त करता है जो मामलों का निपटारा करें। मुकदमे की कार्यवाही में यदि प्रतिवादी (defendant) आरोपों से इनकार करता है, तो वादी (complainant) को गवाहों को प्रस्तुत करना चाहिए या प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। यदि गवाहों के कथनों में विरोधाभास हो, तो राजा को बहुसंख्यक गवाहों की गवाही को निर्णायक मानना चाहिए। यदि कोई गवाह उपलब्ध न हो, तो न्यायाधीशों को जाँच आधारित दृष्टिकोण (investigative approach) अपनाना चाहिए।
प्रमाणों का वर्गीकरण
याज्ञवल्क्य ने प्रमाणों को तीन भागों में वर्गीकृत किया है:
1. लेख्य प्रमाण (Documents)
2. साक्षी (Witnesses)
3. स्वामित्व या वस्तु का अधिकार (Possessions)
यह वर्गीकरण मनु के प्रमाण विषयक विचारों को और अधिक व्यवस्थित करता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और तर्कसंगत बनती है। इस प्रकार मनु का विधि सिद्धांत धर्म, परंपरा और प्रमाण पर आधारित एक समन्वित न्याय व्यवस्था को प्रस्तुत करता है।
प्राचीन काल में भी न्याय राज्य का प्रमुख सद्गुण था। राजा का यह प्रथम कर्तव्य था कि वह राज्य में न्याय स्थापित करे। लगभग सभी स्मृतियों में कानून व्यवस्था और न्याय स्थापित करने कि बात विस्तार से वर्णित है। न्याय व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने के लिए वृहस्पति स्मृति में मनु के सिद्धांतों को और भी परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया गया है।
बृहस्पति ने मनु द्वारा वर्णित 18 विधि शीर्षकों के प्रावधानों को को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया:
1. सिविल (नागरिक) कानून
2. क्रिमिनल (दंडात्मक) कानून।
यह वर्गीकरण हिंदू विधिक परंपरा के विकास में एक बड़ा मील का पत्थर है।
बृहस्पति स्मृति के अनुसार, सिविल कानून (नागरिक विधि) के अंतर्गत जिन विषयों को सूचीबद्ध किया गया है, वे निम्नलिखित हैं:
• धन उधार देना (ऋण देना)
• धरोहर (जमानत या जमा)
• साझेदारी (सहभागिता) के मामलों से जुड़ी चिंताएं
• मजदूरी या वेतन का न मिलना
• भूमि विवाद
• स्वामित्व के बिना बिक्री
• क्रय-विक्रय (खरीद-फरोख्त)
• अनुबंध (वाचा) का उल्लंघन
• पति-पत्नी के संबंध
• चोरी और उत्तराधिकार (विरासत)
• जुआ, जो कि धन से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित है।
इन सभी विषयों का संबंध व्यक्तिगत या सामाजिक धन और संपत्ति से है, अतः इन्हें सिविल मामलों के रूप में वर्गीकृत किया गया।
दूसरी ओर, क्रिमिनल कानून (दंडात्मक विधि) के अंतर्गत वे विषय आते हैं जो किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाते हैं, जैसे:
• दो प्रकार के अपमान (मानहानि)
• हिंसा
• पर-स्त्री से अवैध संबंध, जो कि दूसरों को हानि पहुँचाने वाले कार्य हैं।
वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132-134 के अनुसार चार प्रकार के मामलों को सुप्रीम कोर्ट में अपील के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:
1. संविधान की व्याख्या से संबंधित अपील
2. दीवानी अपील (Civil Appeal)
3. आपराधिक अपील (Criminal Appeals)
4. विशेष अनुमति के साथ की गई अपील (Appeal with Special Permission)
ये चारों प्रकार की प्रक्रियाएँ सिद्धांततः मनु और वृहस्पति स्मृति में वर्णित दीवानी और आपराधिक मामलों से भिन्न नहीं हैं। ये स्मृतियाँ आज के भी कानून और उनके विभाजन का आधार हैं। आज के समय में जिस प्रकार की सामाजिक न्याय (social justice) की अवधारणा है, वह मनु की न्याय संबंधी दृष्टि में पहले से ही समाहित थी। उन्होंने इसे “न्याय का सामाजिक उद्देश्य” (social purpose of justice) कहा, जिसमें राजा का यह कर्तव्य था कि वह उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करे जो स्वयं अपने लिए खड़े नहीं हो सकते हैं।
मनु के अनुसार
• नाबालिग (minor) के उत्तराधिकार (inheritance) और अन्य संपत्ति की रक्षा राजा को तब तक करनी चाहिए जब तक वह गुरुकुल से लौट कर वयस्क न हो जाए।
• राजा को विशेष रूप से अनाथों (orphans), बांझ महिलाओं, बिना संतान वाले पुरुषों, पतियों से रहित स्त्रियों (विधवाओं) तथा रोगग्रस्त महिलाओं की देखभाल करनी चाहिए।
इस प्रकार मनु की न्याय प्रणाली न केवल विधिक न्याय पर बल देती है, बल्कि सामाजिक दायित्व और संवेदनशील शासन की भी वकालत करती है, जो आज के कल्याणकारी राज्य (welfare state) के सिद्धांतों से काफी मेल खाती है। मनु के समय में यह विशाल उपमहाद्वीप विभिन्न जातीय और भाषायी समूहों का निवास स्थान था, जिनकी दृष्टिकोणों और नैतिक मूल्यों में अत्यधिक विविधता थी। मनु इस सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को एक सजीव और संगठित इकाई के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता को भली-भांति समझते थे। मनुस्मृति में जीवन के लगभग सभी पहलुओं—राजनीतिक, आर्थिक, विधिक, सामाजिक आदि—का समावेश है। यह एक विशाल ग्रंथ है, जिसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।
प्राचीन स्मृति शास्त्र और आधुनिक विधिक प्रणाली में वैचारिक अंतर
1. काल-सापेक्षता (Temporal Context):
मनुस्मृति और बृहस्पति स्मृति लगभग 3000 वर्ष पूर्व की सामाजिक, धार्मिक, और नैतिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर रची गई थीं। उन शास्त्रों में उस समय की समाज संरचना, दोष भावना (guilt psychology), धर्म, और सामाजिक उत्तरदायित्व की छवि झलकती है, जो आज की अपेक्षा एकदम अलग थी।
2. समाज-केन्द्रित बनाम व्यक्ति-केन्द्रित दृष्टिकोण:
स्मृति शास्त्रों में समाज के हित और धर्म-अनुशासन को प्रमुखता दी गई है, जबकि आधुनिक कानून, जैसे भारतीय संविधान, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, और अधिकारों पर आधारित है।
3. नियमों की स्थिरता बनाम परिवर्तनशीलता:
भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत हुआ था और तब से अब तक उसमें अनेक बार संशोधन हो चुका है। यदि केवल 70-72 वर्षों में ही समाज और समस्याएं इतनी बदल सकती हैं, तो 3000 वर्ष पूर्व की व्यवस्था को शब्दश: आज की कसौटी पर जाँचना न्यायसंगत नहीं होगा।
4. तत्कालीन न्यायिक प्रणाली की गहराई:
आचार्य मनु और बृहस्पति ने उस समय की न्यायिक व्यवस्थाओं को विस्तृत रूप से परिभाषित किया। मनु ने धर्म के मूल तत्वों के अनुसार राजधर्म और न्याय का निर्धारण किया, वहीं बृहस्पति ने न्यायालयों की विभिन्न श्रेणियाँ, साक्ष्य के प्रकार, और सिविल व क्रिमिनल कानून के वर्गीकरण जैसे आधुनिक तत्वों को आधार बनाया।
मनु धर्म और राजनीति को सततता के उपकरण (instruments of continuity) के रूप में प्रयोग करके, जीवन को आदर्श रूप से स्थापित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु दिशा देने का कार्य करते हैं। यह ग्रंथ प्राचीन भारत के एक महान चिंतक की नैतिक दृष्टि की अभिव्यक्ति है, जो व्यावहारिकता (pragmatism) और आदर्शवाद (idealism)—दोनों को समान रूप से महत्व देता है।
के. श्रीरंजनी सुब्बा राव ने अपने लेख “Manu’s Ideas on Administration” (मनु के प्रशासन संबंधी विचार) में कहा है कि — मनु के प्रशासन संबंधी विचार आधुनिक प्रशासनिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण की अवधारणा को प्रतिबिंबित करते हैं। यही शायद इस ग्रंथ की सबसे विशिष्ट विशेषता है—इसमें एक ओर जहाँ सार्वभौमिकता (universality) की झलक है, वहीं दूसरी ओर यह कालातीत होते हुए भी विशिष्टताओं के साथ संतुलन बनाए रखता है।