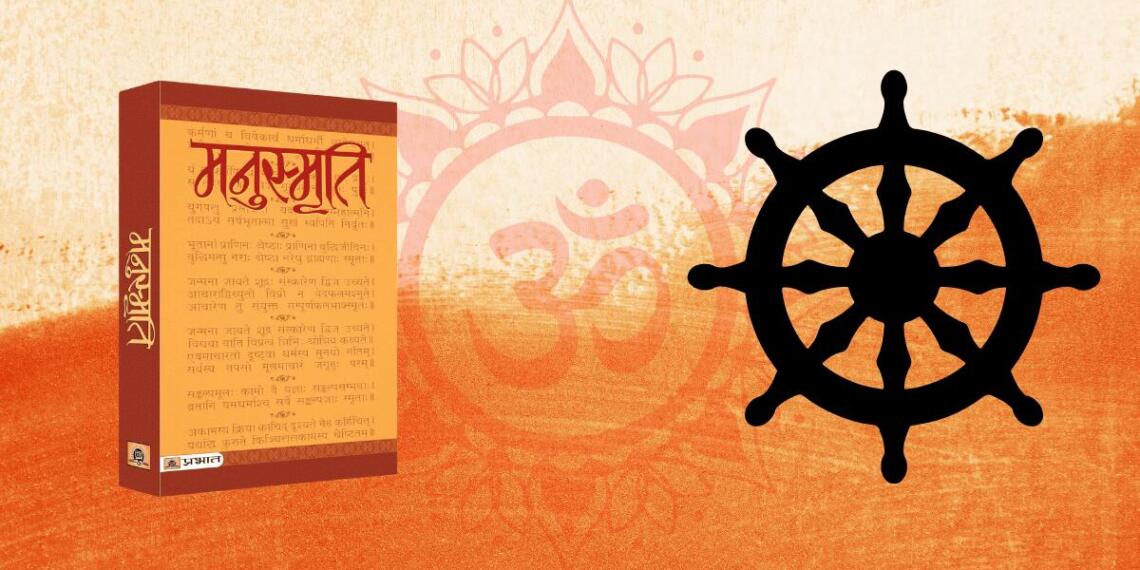स्मृतियों में सबसे प्राचीन, श्रेष्ठ एवं प्रमुख मानव स्मृति को माना गया है। ऋग्वेद में “मनु” को मानव जाति का पिता, प्रथम यज्ञ कर्ता तथा संहिता का प्रवर्तक कहा गया है। शास्त्र ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ से लेकर अनेक मन्वंतर हुए हैं, जिनमें भिन्न–भिन्न मनुओं का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति में उल्लिखित है कि “मनु” कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक परंपरा है। वायु पुराण में भी विभिन्न मनुओं के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार, आयुर्वेद एवं अन्य ग्रंथों में भी विभिन्न युगों में भिन्न–भिन्न मनुओं के अस्तित्व की चर्चा की गई है। विदुरनीति के अनुसार मनु ही विश्व के प्रथम संविधान रचयिता हैं। वेदों में सूत्र रूप में जो कुछ उल्लिखित है, उसकी विस्तृत व्याख्या स्मृतिग्रंथों में की गई है। स्मृतियाँ वेदों के गूढ़ ज्ञान का व्यवहारिक एवं क्रियात्मक रूप हैं। इनमें मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए आचार एवं व्यवहार का निर्धारण किया गया है, इसलिए इन्हें आचार संहिता कहा जाता है। मुख्यतः बारह स्मृतियाँ जिनमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, दक्ष स्मृति, व्यास स्मृति, कात्यायन स्मृति, लघु हारीत स्मृति, विष्णु स्मृति तथा शंख स्मृति हैं जो सुलभता से उपलब्ध हैं। शेष स्मृतियाँ विभिन्न संग्रह ग्रंथों एवं भाष्यों में वर्णित हैं। स्मृतियाँ तत्कालीन समय की आचार संहिताएँ थी जिनमे समय समय पर परिवर्तन की भी अपेक्षा थी। यही विशेषता इनको अधिक प्रगतिशील बनाती है।
डॉ० पी.वी. काणे के अनुसार ‘धर्म’ शब्द की उत्पत्ति ‘धृ’ धातु से हुई है जिसका अर्थ है- धारण करना। महाभारत के कर्ण-पर्व के अनुसार धारण करने वाले को धर्म कहते हैं। धर्म प्रजा को धारण करता है –
धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः।
यत्स्याद्धारणसंयुक्त स धर्म इति निश्चयः।। महाभारत कर्णपर्व, ३,२१,४१
इस प्रकार धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है। धर्म का आशय नैतिकता तथा सद्आचरण से है। मनुस्मृति भी धर्म के संबंध में इसी आचरणगत विचार को अंगीकार करती है।
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियं आत्मनः ।
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ।।
मनुस्मृति में वेद, स्मृति, सदाचार और अपनी आत्मा की प्रियता—इन चारों को धर्म के लक्षण कहा गया है।
- वेद (श्रुति) – यह शाश्वत एवं दिव्य ज्ञान का स्रोत है, जो सत्य और धर्म का मूल आधार माना जाता है।
- स्मृति – वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ, जो आचार–संहिता और सामाजिक नियमों को स्पष्ट करते हैं।
- सदाचार – समाज में प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ आचरण करने वाले महान व्यक्तियों की परंपरा, जो नैतिकता और आदर्शों पर आधारित होती है।
- आत्मनः प्रियं (स्वात्मसंतोष) – व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होने वाला आत्मिक संतोष, जो उसे अपने कर्तव्य और नैतिकता का बोध कराता है।
ये चारों तत्व ही धर्म का आधार हैं और व्यक्ति के जीवन में संतुलन एवं सदाचार की स्थापना करते हैं। इस प्रकार धर्म आचरण का पर्याय है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण भी बताए गए हैं –
धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्॥
दशलक्षणानिधर्मस्ययेविप्राःसमधीयते।
अधीत्यचानुवर्तन्तेतेयान्तिपरमांगतिम्।।
दशलक्षणकंधर्मंअनुतिष्ठन्समाहितः।
वेदान्तंविधिवच्छ्रुत्वासंन्यसेदनृणोद्विजः।।
अर्थात् धैर्य, क्षमा, संयम, अस्तेय, पवित्रता, इन्द्रिय निग्रह, धी या बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना– ये धर्म के दस लक्षण कहलाते है। धर्म के दश लक्षणों का जो द्विज अध्यन – मन न करते हैं और पढ़कर – मनन करके इनका पालन करते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। मनुस्मृति में “आचारः परमो धर्मः“ कहकर आचार (व्यवहार) को ही परम धर्म बताया गया है। अर्थात्, वेदों और स्मृतियों में वर्णित आचार ही सर्वोच्च धर्म है। इसलिए आत्मा के कल्याण के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इस आचार का पालन निरंतर करना चाहिए।
मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करती है पर यहाँ जन्मजात जाती व्यवस्था के बजाय कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। महर्षि मनु के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य “द्विज“ होते हैं। द्विज का अर्थ है जिसका दो बार जन्म हुआ हो अर्थात्, जन्म के समय मनुष्य अज्ञान और अशिक्षा के कारण साधारण स्थिति में होता है तो वह शूद्र की श्रेणी में आता है। जब वह वेदाध्ययन और ज्ञानार्जन करता है, तब उसका द्वितीय जन्म होता है, इसलिए उसे द्विज कहा जाता है। मनुस्मृति के अनुसार जन्म से सभी शूद्र ही होते हैं परंतु संस्कार और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्म अर्थात परमतत्व के साक्षात्कार का अधिकारी हो जाता है।
जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते।
वेदपाठाद् भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः।।
भगवद्गीता मे ब्राह्मण के गुणो का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवद्गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में इनके गुणों का वर्णन किया गया है,
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च।
ज्ञानंविज्ञानमास्तिक्यंब्रह्मकर्मस्वभावजम्।।
अर्थात इन सभी गुणों को स्वाभाव से पालन करने वाला ही ब्राह्मण है अर्थात ब्रह्म भाव वाला है। मनुस्मृति इस बात को स्वीकार करती है कि अपने कर्मो से कोई भी किसी वर्ण का व्यक्ति ब्रह्म भाव को अपना सकता है और कोई ब्राह्मण अपने कर्म से शूद्र हो सकता है। जो ब्राह्मण अपने आचरण से भ्रष्ट हो जाता है, वह वेदाध्ययन का फल प्राप्त नहीं करता। अर्थात्, केवल वेद पढ़ने से ही लाभ नहीं होता, बल्कि इसके लिए शुद्ध आचरण भी आवश्यक है। इसके विपरीत, जो ब्राह्मण सदाचार का पालन करता है, वह वेदों में वर्णित समस्त फलों का अधिकारी बनता है क्योंकि वेदों का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान एवं आचरण की शुद्धता है, न कि मात्र पठन–पाठन। अतः आचरण ही धर्म का मूल तत्व है और सदाचारी व्यक्ति ही वेदज्ञान के वास्तविक फल का अधिकारी होता है। वैदिक ऋषि–मुनियों ने अपने अनुभव से यह जाना कि आचरण (व्यवहार) से ही धर्म की गति संभव है। यदि आचरण शुद्ध न हो, तो धर्म न ही स्थिर रह सकता है और न ही आगे बढ़ सकता है। मनुष्य को अपने आत्मिक और नैतिक उत्थान के लिए सदाचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही धर्म का सर्वोच्च स्वरूप है।
धर्म किसी संकीर्ण परिभाषा या बंधन में नहीं बंधा है, बल्कि यह आचरण और कर्तव्य का एक व्यापक दृष्टिकोण है। कात्यायन स्मृति के अनुसार, वेदों में छह अंग माने गए हैं—
- शिक्षा (Phonetics – उच्चारण शास्त्र)
- कल्प (Rituals – विधि विधान)
- व्याकरण (Grammar – भाषा का शुद्ध प्रयोग)
- निरुक्त (Etymology – शब्दों की व्याख्या)
- छंद (Metrics – छंद शास्त्र)
- ज्योतिष (Astronomy – खगोलीय गणना)
ये सभी वेद के पूरक माने गए हैं, जो धर्म और आचरण की स्पष्टता के लिए आवश्यक हैं। इसी कारण, धर्म केवल ज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहार में अपनाया गया कर्तव्य है। मनुष्य को अपने कर्मों के आधार पर पाप और पुण्य का फल प्राप्त होता है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार, “पाप” वे कर्म हैं जो नैतिक और सामाजिक दृष्टि से निंदनीय हैं, जबकि “पुण्य” वे कर्म हैं जो आत्मा की उन्नति और समाज के कल्याण के लिए किए जाते हैं। मनुस्मृति मे पाप और पुण्य का विस्तार से वर्णन किया गया है।
मनुस्मृति के अनुसार पाप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला महापाप, जिसमें ब्रह्म हत्या अर्थात गुरु या ज्ञानी की हत्या, मद्यपान या किसी भी प्रकार के नशे की लत, ब्रह्मचर्य भंग यानी असंयमित जीवन व्यतीत करना, माता-पिता का अपमान, तथा छल, धोखा और भ्रष्ट आचरण शामिल हैं। दूसरा लघु पाप, जिसमें झूठ बोलना, चोरी करना, व्यर्थ की हिंसा करना और असत्य आचरण करना आता है।
पुण्य कर्म वे होते हैं जो आत्मा की शुद्धि और समाज के कल्याण के लिए किए जाते हैं। इन्हें चार प्रमुख भागों में बाँटा जा सकता है। पहला सत्कर्म, जिसमें अच्छे कर्म करना और परोपकार करना शामिल है। दूसरा दान, जो जरूरतमंदों की सहायता करने से संबंधित है। तीसरा तपस्या, जिसमें आत्मसंयम और साधना का अभ्यास किया जाता है। चौथा भक्ति, जिसमें ईश्वर की आराधना और श्रद्धा भाव से किया गया उपासना कर्म शामिल है।
मनुस्मृति में धर्म के सम्यक पालन के लिए इसे कई भागों मे विभक्त किया गया है-
सामान्य धर्म: इसके अंतर्गत मनुष्य के सांसारिक कर्तव्यों को रखा जाता है । जो एक मनुष्य को परिवार , समाज और देश के प्रति उसके ज़िम्मेदारियों का पालन करने को प्रेरित करता है। जैसे, पिता धर्म ( पिता के रूप में कर्त्तव्य ), पुत्र धर्म (पुत्र के रूप में कर्त्तव्य) इत्यादि।
विशिष्ट धर्म: इसके अंतर्गत रीति-रिवाज, परंपराओं , ईश्वर के प्रति विश्वास , पारलौकिक मान्यताओं को रखा जा सकता है । जो मनुष्य को नैतिकता और पवित्र आचरण का पालन करवाती है ।
आपद्धर्म: संकटकाल में अपनाए गए कर्त्तव्य को आपद्धर्म कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप किसी ब्राह्मण को लेते है यदि उसका भरण-पोषण कर्मकांड अथवा पूजा-पद्धति द्वारा संभव ना हो तो इस दशा में वह क्षत्रियोचित या वैश्य संबंधी कार्य कर अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकता है। इसे ही आपद्धर्म कहते है।
गुणवाचक धर्म: इसका संबंध प्रकृति या स्वभाव को दर्शाने के लिए स्वीकार किया जाता है । जैसे, पानी का धर्म है शीतलता, आग का धर्म है, उष्णता प्रदान करना इत्यादि।
इस प्रकार धर्म भारतीय परंपरा में सभी मत मतांतरों द्वारा आचार संहिता के रूप में ही परिभाषित किया जाता रहा है। मौर्यवंशीय शासक अशोक ने धम्म (धर्म) को एक व्यावहारिक और नैतिक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया। अपने दूसरे स्तंभलेख में वह स्वयं प्रश्न करता है— “कियं चु धम्मेति?” (धम्म क्या है?)। इसके उत्तर में, अपने दूसरे और सातवें शिलालेख में वह स्पष्ट करता है— “अपासिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचये मादवे साधवे च”। अर्थात धम्म वही है जिसमें कम पाप किया जाए, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, दया और दान की भावना हो, सत्य का पालन किया जाए, जीवन पवित्रता से भरा हो, स्वभाव में मधुरता और सरलता बनी रहे तथा सद्गुणों को अपनाया जाए। महाभारत के वनपर्व (३१३/१२८) में कहा है-
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥
– मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश, और रक्षित धर्म रक्षक की रक्षा करता है। इसलिए धर्म का हनन कभी न करना, इस डर से कि मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले।