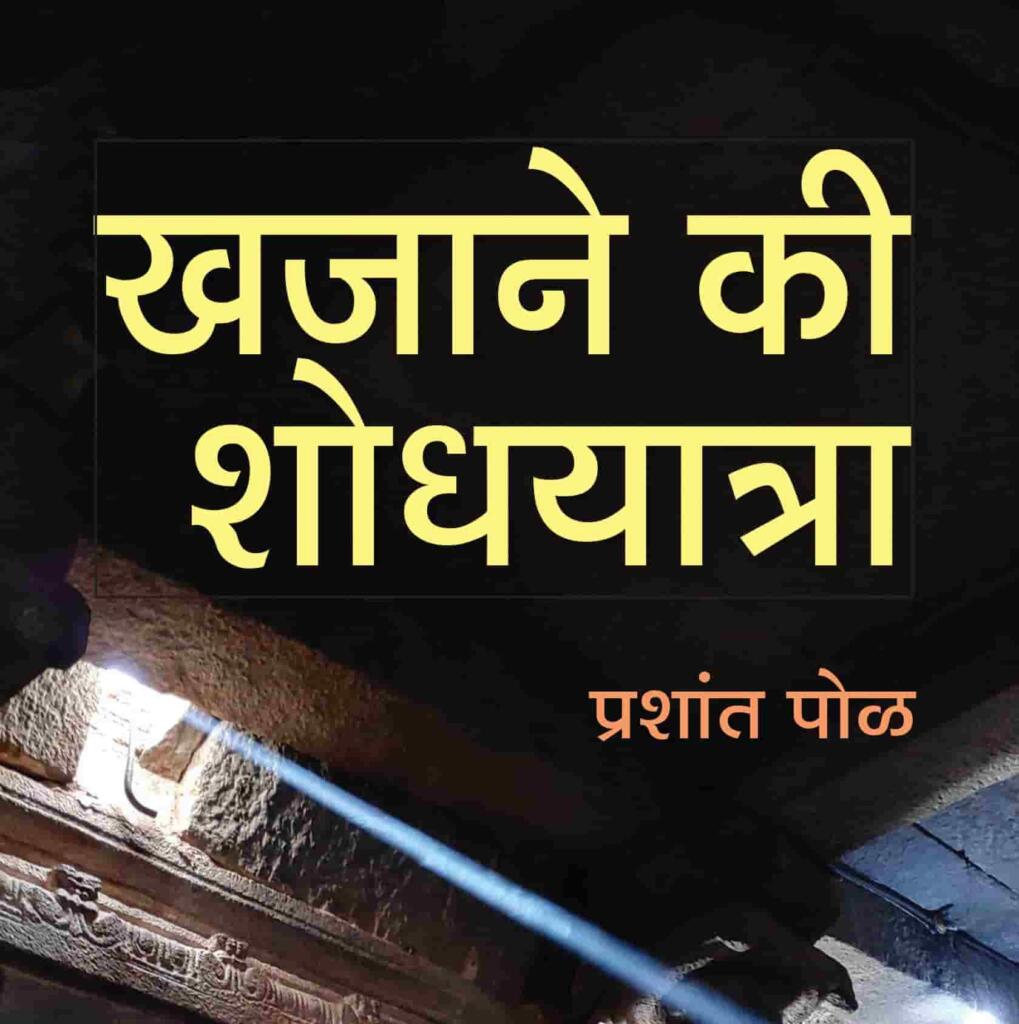पुस्तक का नाम: खजाने की शोधयात्रा
लेखक: प्रशांत पोल
प्रकाशक: प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
पृष्ठ: 221
क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन स्टेडियम कहाँ है? या आजकल मोबाइल फोन पर खेला जाने वाला बहुत लोकप्रिय खेल ‘लूडो’ का असली नाम क्या है? पत्तों (कार्ड्स) के साथ खेले जाने वाले ‘ताश’ के खेल का उद्गम स्थल कहाँ है, इसका वास्तविक नाम क्या है? क्या आप जानते हैं कि यंत्रमानव (रोबोट) की प्रथम परिकल्पना कहाँ हुई थी या किसने की थी? ऐसे और भी अनेक प्रश्न मेरे सामने हैं। हो सकता हैं आप में से अधिकांश लोग इन प्रश्नों के उत्तर जानते हों, लेकिन यह सत्य है कि मुझे इनके उत्तर पता नहीं थे ! तीन शब्दों में यदि उत्तर देना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है “भारतीय ज्ञान परंपरा” में।
कोई भी कह सकता है कि लूडो या ताश के पत्ते या फिर रोबोट का भारतीय ज्ञान परंपरा से क्या संबंध? मेरे मन में भी यही प्रश्न उठा था, लेकिन जब ‘खजाने की शोध यात्रा’ पुस्तक पूरी पढ़ ली, तब समझ आया कि अभी बहुत कुछ जानना, समझना बाकी है या दूसरे शब्दों में कहूँ तो ज्ञान के खजाने की लंबी शोध यात्रा करना शेष है।
‘खजाने की शोध यात्रा’ पुस्तक लिखी है सुप्रसिद्ध लेखक ‘प्रशांत पोल’ ने, जिनकी ‘वे पन्द्रह दिन’ पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और उनकी ही लिखी ‘भारतीय ज्ञान का खजाना’ पुस्तक भी बहुत लोकप्रिय हुई है। ‘खजाने की शोध यात्रा’ पुस्तक का प्रकाशन किया है सुप्रसिद्ध प्रकाशक ‘प्रभात’ प्रकाशन ने। भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्ध धरोहर की खोज और अविष्कार को केंद्र में रखने वाली इस पुस्तक में 18 अध्याय और 221 पृष्ठ हैं। लेखन शैली बहुत सरल और प्रभावशाली है।
पुस्तक की भूमिका अपने आप में एक शोध परिकल्पना (हाइपोथिसिस) जैसी है। ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह पाठक को पूरी पुस्तक को एक बार में पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें उस सत्य को स्वीकार करने का साहस किया गया है जिसे स्वीकार करने में शायद भारतीय जनमानस को दिक्कत हो सकती है। भूमिका से ऐसा ही एक अंश यहाँ उद्धृत करना उचित रहेगा, “यह पुस्तक लिखते समय ‘पुराना है तो ही सब सुहाना है’ या ‘मात्र भारतीयों के पास ही सब कुछ ज्ञान था’ ऐसी मेरी भूमिका नहीं थी। यह उचित भी नहीं है। किंतु यह भी सत्य है कि कुछ हजार वर्ष पूर्व अपना भारत विश्व में सर्वाधिक समृद्ध, संपन्न और ज्ञानवान देश था।”
4 पृष्ठों की इस छोटी सी भूमिका में कुछ ऐसा भी लिखा है जो पाठक को सोचने पर विवश करेगा। इसके लिए लेखक ने लिखा है, “एक बात जो दिल को कचोट रही थी ……यह हमारा दुर्भाग्य है।” कुल मिलाकर यह भूमिका इस पुस्तक को पूरा पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला एक उचित और प्रभावी ‘कैटेलिस्ट’ है।
इस पुस्तक में ऐसी अनेक अज्ञात या अनछुई बातों को अत्यंत रोचक शैली में सामने लाने का उत्कृष्ट प्रयास किया गया है। जैसे-जैसे पाठक अध्याय-दर-अध्याय पढ़ते हुए आगे बढ़ेगा उसे ‘गौरव की अनुभूति’ भी होगी और ‘पछतावा’ भी होगा। जहाँ तक भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति की बात है तो इसके पीछे के कारण सार्वजनिक हैं। लेकिन ‘पछतावा’ इस कारण से होगा कि इतना विपुल ज्ञान भंडार होने के बावजूद कोई ढंग का शोध क्यों न हुआ, आज भी पाश्चात्य जगत के उदाहरण या संदर्भ क्यों लिए जाते हैं? ऐसा विपुल खजाना कहाँ और कैसे विलुप्त हो गया? ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की गयी? लेखक के शब्दों में कहें तो आधुनिकता का डंका बजाने के बाद भी हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारे संचित को, हमारी विरासत को हम ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं।
पुस्तक का प्रत्येक अध्याय नवीन ‘शोध’ के लिए आवाहन जैसा प्रतीत होता है। हर अध्याय एक नया विषय छेड़ता है, नई जानकारी प्रदान करता है और वही गौरव की अनुभूति के साथ साथ पछतावा होता है। आखिर क्यों हम ये सब न कर पाए !
पुस्तक का अध्याय 10 तो एक स्तर ऊपर जाकर झटके देता है। इसमें पाठक जान पायेगा कि ‘यंत्रमानव’ जिसे अंग्रेजी भाषा में ‘रोबोट’ कहा जाता है, उसकी परिकल्पना ‘समरांगण सूत्रधार’ नामक ग्रन्थ में बिलकुल स्पष्ट रूप से दी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमें यही बताया गया या पता है कि रोबोट की संकल्पना विदेशियों ने की है। इस अध्याय के अंत में लेखक ने जो लिखा है वह मन कचोटता है, “मेरी जानकारी के अनुसार भारत में केवल दो ही लोगों ने इस विषय पर पीएचडी की है। हमें अपने ही ज्ञान की महत्ता का पता नहीं, यह हमारा दुर्भाग्य है।”
मनुस्मृति को लेकर आजकल बड़ा बबाल होता रहता है। इस तरह का वातावरण बनाया जाता है कि मानों भारत की सभी व्यवस्थायें मनुस्मृति के आधार पर ही चलती आई हैं। यह पुस्तक इस भ्रान्ति का निवारण भी अत्यंत प्रमाणिकता के साथ करती है। अत्यंत सरल भाषा में लिखी इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय पर पृथक समीक्षा लिखी जा सकती है, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पुस्तक का अंतिम अध्याय पाठक को विघ्नहर्ता श्री गणेश के माध्यम से सनातन अथवा हिन्दू संस्कृति की विराटता या वैश्विक व्यापकता के बारे में अत्यंत रोचक जानकारी प्रदान करेगा।
संक्षेप में कहें तो यह ‘खजाने की शोधयात्रा’ पुस्तक वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा के खजाने पर शोध करने हेतु भारत को भारत की दृष्टि से देखने वालों के लिए आह्वान है। हर आयु वर्ग का पाठक इससे लाभान्वित होगा और युवा वर्ग तो इससे प्रेरणा लेकर उस ज्ञान के खजाने के अंतिम बिंदु तक पहुंचने का पथिक बन सकता है।
नारायणायेती समर्पयामि ….