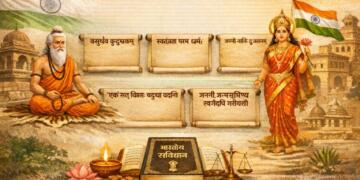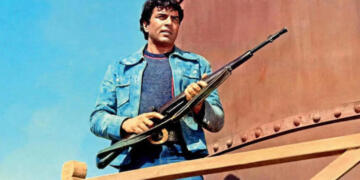अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के कथित नैतिक ताने-बाने को हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध से पैसा बना रहा है, क्योंकि नाटो देश अमेरिकी हथियार खरीद रहे हैं। यह टिप्पणी सीधे उस पश्चिमी नैरेटिव को चुनौती देती है, जिसके तहत भारत पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि रूस से तेल खरीदकर वह पुतिन की युद्ध मशीन को ताक़त देता है।
प्रश्न यह है कि जब वाशिंगटन खुद मान रहा है कि वह हथियारों की बिक्री से मुनाफ़ा कमा रहा है, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी खरीद को युद्ध का ईंधन क्यों बताया जाता रहा है? अगर यह सही भी है तो इसमें गलत क्या है। सवाल यह कि अमेरिका और नाटो देश भी तो यूक्रेन को युद्ध के लिए समर्थन और हथियार दोनों दे रहे हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये देश अगर युक्रेन को मदद न करते तो यह युद्ध तो कब का समाप्त हो चुका होता। तो क्या इसके लिए वे दोषी नहीं हैं।
अमेरिकी हथियार उद्योग और युद्ध की अर्थव्यवस्था
जानकारी हो कि अमेरिका का रक्षा उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा है। स्टॉकहोम स्थित SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 2015-19 और 2020-24 के बीच अमेरिकी हथियार निर्यात में 21% की वृद्धि हुई है। इससे उसकी वैश्विक हिस्सेदारी 43% तक पहुंच गई है। इस दौरान रूस का निर्यात घटकर लगभग 64% कम हो गया (SIPRI, 2025)।
यूरोप के नाटो देशों ने रूस—यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अपने रक्षा बजट दोगुने-तिगुने कर दिए हैं। पोलैंड ने अमेरिकी HIMARS रॉकेट सिस्टम और F-35 फाइटर जेट्स खरीदे और जर्मनी ने मिसाइल रक्षा प्रणाली का बड़ा करार किया। यही कारण है कि ट्रंप ने कहा कि “अमेरिका पैसे कमा रहा है।” साफ शब्दों में कहें तो यह युद्ध अमेरिकी कंपनियों—लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन और बोइंग के लिए मुनाफा कमाने का बड़ा अवसर बन चुका है। वे कमा भी रहे हैं।
भारत की ऊर्जा सुरक्षा की मजबूरी
यहीं पर भारत की स्थिति कुछ अलग है। जानकारी हो कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। वह अपनी 85% ज़रूरतें विदेश से पूरी करता है। आंकड़ों के आधार पर बात करें तो युद्ध से पहले रूस से उसका आयात 2% से भी कम था। लेकिन 2022 के बाद रूस ने यूरोपीय बाजार खोने पर भारत को भारी छूट पर तेल बेचना शुरू कर दिया। IEA (International Energy Agency) की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में भारत ने रूस से लगभग 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन (mb/d) तेल आयात किया, जो उसके कुल आयात का 38% था (IEA, 2024)। इससे भारत को महंगाई पर नियंत्रण रखने और अरबों डॉलर बचाने में मदद मिली।
Reuters के मुताबिक जुलाई 2025 में भी भारत का रूसी तेल आयात करीब 1.5 mb/d रहा, यानी कुल आयात का लगभग 34% (Reuters, 2025)। इससे साफ है कि भारत ने रूस से तेल खरीद को आर्थिक व ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी कदम माना, न कि युद्ध को राजनीतिक समर्थन।
पश्चिम का पाखंड और दोहरे मानदंड
यहीं पर पश्चिम का दोहरा रवैया उजागर होता है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह कि भारत जो तेल खरीदता है, वह नागरिक उपभोग और विकास की ज़रूरत है। लेकिन, अमेरिका जो हथियार बेचता है, वह तो सीधे युद्ध और विनाश का साधन है। लेकिन पश्चिम का नैरेटिव अलग है। अमेरिका और यूरोपीय संघ बार-बार कहते हैं कि भारत का तेल आयात रूस को युद्ध के लिए राजस्व देता है। परंतु, अमेरिकी हथियार बिक्री को वे “लोकतंत्र की रक्षा” और “स्वतंत्रता की लड़ाई” के नाम पर वैध ठहराते हैं। यह दोहरा रवैया क्यों?
Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) के अनुसार, फरवरी 2022 के बाद से भारत रूस के कुल कच्चे तेल निर्यात का 20% से अधिक खरीदार रहा है (CREA, 2024)। लेकिन उसी अवधि में अमेरिका और यूरोप के हथियार सौदे कई गुना बढ़े हैं और इनका असर सीधा युद्ध को लंबा करने पर पड़ता है। इसलिए उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
वैसे अमेरिका के लिए यह कोई नई बात नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी उद्योग ने यूरोप और एशिया के देशों में हथियार बेचकर भारी कमाई की। शीत युद्ध के दौर में भी वियतनाम, अफगानिस्तान और मध्य-पूर्व अमेरिकी कंपनियों के अनुबंधों से भर गए। इराक युद्ध (2003) और अफगानिस्तान में दो दशक तक चले सैन्य अभियानों ने हथियार कंपनियों और निजी कॉन्ट्रैक्टर्स को अरबों डॉलर दिए। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने 1961 में चेतावनी दी थी कि “मिलिट्री-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स” लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। आज तो ट्रंप का यह बयान उस चेतावनी की पुष्टि करता हुआ लगता है।
भारत का पक्ष और कूटनीति
वैसे भारत बार-बार कह चुका है कि उसका तेल आयात राजनीतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक निर्णय है। भारत का इतना बड़ा उपभोक्ता वर्ग महंगे तेल पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर भारत ने रूस से तेल न खरीदा होता तो महंगाई आसमान छू लेती और विकास दर पर गंभीर असर पड़ता। इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही होतीं।
दिलचस्प यह भी है कि भारत से रिफाइन होकर बने पेट्रोल और डीज़ल यूरोप को भी निर्यात होते हैं। यानी परोक्ष रूप से वही यूरोपीय देश, जो भारत की आलोचना करते हैं, उसी रूसी तेल से बने उत्पाद का ही उपयोग करते हैं। भारत ने तटस्थता की नीति अपनाते हुए युद्ध पर संवाद और शांति की पैरवी की है। भारत के लिए प्राथमिकता अपनी जनता की भलाई और ऊर्जा सुरक्षा है। वह ऐसा क्यों न करे?
ट्रंप ने अनजाने में ही सही, अमेरिकी पाखंड को उजागर तो कर ही दिया है। जब अमेरिका खुद मान रहा है कि वह युद्ध से मुनाफ़ा कमा रहा है, तो उसके पास भारत पर उंगली उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचता। भारत के लिए यह सबक है कि उसे अपनी स्थिति और स्पष्टता से दुनिया के सामने रखनी चाहिए। तेल खरीदना और हथियार बेचना एकसमान नहीं हैं। भारत यह कदम अपनी जनता की ज़रूरत के लिए उठा रहा है, जबकि अमेरिका का मकसद लाभ और भू-राजनीतिक दबदबा है।
आज के समय की बात करें तो आधुनिक युद्ध सिर्फ़ रणभूमि पर ही नहीं, बल्कि बाज़ार और उद्योगों में भी लड़े जाते हैं। यूक्रेन युद्ध इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। अमेरिका का हथियार उद्योग इस युद्ध से फल-फूल रहा है, रूस का तेल उद्योग उसकी रीढ़ है। ऐसे में भारत जैसे देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए व्यावहारिक कदम उठा रहे हैं। इसमें गलत क्या है?
लेकिन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भारत के खिलाफ उनके इस नैरेटिव को उलट देता है। ट्रंप ने मान लिया कि अमेरिका युद्ध से “कमाई” कर रहा है। ऐसे में उनका यह कहना कि भारत का तेल आयात युद्ध को ईंधन देता है, यह तो सिर्फ़ पश्चिमी पाखंड ही है। असली सवाल यही है कि युद्ध को लंबा खींचने वाला कौन है—वह जो तेल खरीदकर अपनी जनता को राहत देता है, या वह जो बम और मिसाइल बेचकर मुनाफ़े की राजनीति करता है?