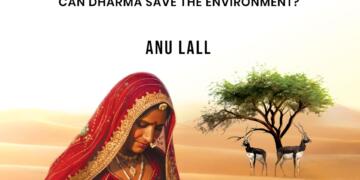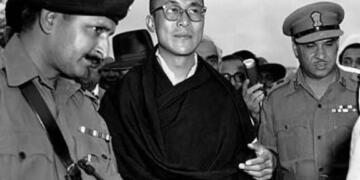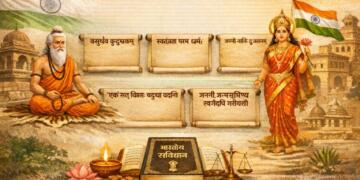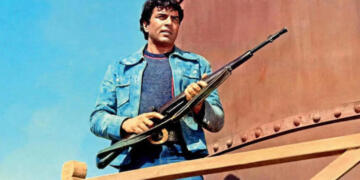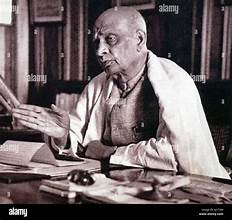31 अक्टूबर 2025 को पूरा भारत सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। लौहपुरुष के रूप में विख्यात सरदार पटेल केवल स्वतंत्र भारत के संगठनकर्ता नहीं थे, वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने जीवन के हर निर्णय में राष्ट्रभक्ति को सर्वोपरि रखा। उनके व्यक्तित्व की महानता यह थी कि सत्ता, पद या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कभी उनके मार्गदर्शन का आधार नहीं बनी। आज का भारत जिस सीमा, संगठन और स्थिरता में है, उसमें उनकी दूरदर्शिता और निर्णय क्षमता का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
सरदार पटेल का जीवन हमेशा संघर्ष और संगठन के बीच पला-पोसा। गृहमंत्री बनने से पहले वे स्वतंत्रता संग्राम के हर मोर्चे पर सक्रिय थे। स्थानीय संगठनों की शक्ति को एक मजबूत राष्ट्रीय नेटवर्क में बदलना उनका स्वभाव था। वे अक्सर अपने सहयोगियों से कहते थे, नेता वही है जो जनता की भाषा समझे और उसका विश्वास जीते। इसी दृष्टि ने उन्हें प्रांतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वमान्य नेता बना दिया।
उनकी नेतृत्व क्षमता केवल प्रशासनिक निर्णय तक सीमित नहीं थी। उनके फैसले अक्सर कठिन और साहसिक होते थे। 1946 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के समय, जब पटेल निर्विरोध चुने गए थे, तब उन्होंने साफ कर दिया था कि उनका उद्देश्य पद नहीं, बल्कि राष्ट्रहित है। यह निर्णय उनकी दूरदर्शिता और नैतिक मजबूती को दर्शाता है।
गांधीजी और पटेल का गहन संबंध
गांधीजी ने कई बार माना कि उन्हें नेहरू अत्यंत प्रिय थे, लेकिन प्रशासन और संगठन के मामले में सरदार पटेल सर्वश्रेष्ठ थे। गांधीजी अक्सर अपने सहयोगियों से कहते थे, यदि प्रशासनिक कार्य की दक्षता चाहिए, तो पटेल को देखो। यह प्रशंसा केवल औपचारिक नहीं थी, गांधीजी जानते थे कि भारत की एकता और संगठनात्मक मजबूती की जिम्मेदारी पटेल के हाथ में सुरक्षित है।
गांधीजी की हत्या के बाद राजनीतिक परिस्थितियां अत्यंत संवेदनशील थीं। कुछ विरोधी यह फैलाने लगे कि पटेल ने गांधीजी की सुरक्षा में विफलता दिखाई और वे प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। इस अफवाह से प्रभावित होकर सरदार पटेल ने इस्तीफा देने तक की पेशकश कर दी। लेकिन, नेहरू ने उनसे कहा, आप पर भरोसा है, वल्लभभाई। देश की सेवा में आपका योगदान किसी भी पद से बड़ा है। इसके बाद सरदार पटेल ने उस समय समझा कि राष्ट्रहित व्यक्तिगत महत्व से ऊपर है।
मौलाना आजाद और मुस्लिम नेताओं के साथ संतुलन
1939 में मुस्लिम लीग द्वारा धार्मिक आधार पर विभाजन की कोशिशों के दौरान गांधीजी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। उनका यह कदम न केवल राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए था, बल्कि यह दिखाता है कि पटेल जैसे नेता हमेशा बड़ी तस्वीर को समझते थे। वे जानते थे कि धार्मिक और सामाजिक संतुलन के बिना भारत की स्वतंत्रता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है।
मौलाना आजाद ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश दूतावासों और विभिन्न वार्ताओं में किया। पटेल ने इस दौरान कभी उनकी आलोचना नहीं की। उन्होंने संगठन को प्राथमिकता दी और व्यक्तिगत महत्व को पीछे रखा। उनके निर्णय हमेशा राष्ट्रहित के लिए थे, चाहे वह रियासतों का विलय हो या राजनीतिक संतुलन बनाए रखना।
1946 का कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव और पद का बलिदान
1946 आते-आते स्वतंत्रता की संभावना स्पष्ट हो चुकी थी। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाला नेता ही अंतरिम सरकार बनाने का आमंत्रण प्राप्त करता। सरदार पटेल इस समय निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। लेकिन राजनीति ने एक मोड़ लिया। उनके विरोधी तंत्र ने नेहरू को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश किया।
उस समय नेहरू ने स्पष्ट कर दिया कि वे केवल नंबर वन बनना चाहते हैं। यह सुनकर पटेल ने अपने व्यक्तिगत महत्व और आकांक्षाओं को पीछे रखा और राष्ट्रहित के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया। बेशक इसमें गांधीजी की भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी। पटेल के इस निर्णय पर राजेंद्र प्रसाद ने दुःख व्यक्त किया और समझाया कि गांधीजी ने नेहरू के पक्ष में पटेल से बलिदान करवाया है।
इस पर सरदार पटेल ने अपने निर्णय की व्याख्या अपने सहयोगियों से कुछ इस तरह की: नेता वही है जो पद से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को देखे। अगर मैं अपनी महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता देता, तो देश को जो स्थिरता चाहिए थी, वह संभव नहीं होती। यह शब्द उनके चरित्र की गहराई को दर्शाते हैं।
भारत की एकता और रियासतों का विलय
सरदार पटेल का नेतृत्व भारत की एकता के लिए निर्णायक रहा। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर में रियासतों का विलय उनके दूरदर्शी फैसलों का ही परिणाम था। उनके निर्णय हमेशा संतुलित और न्यायसंगत होते थे। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने व्यक्तिगत भावनाओं या धार्मिक आधार पर कभी निर्णय नहीं लिया।
उदाहरण के लिए, हैदराबाद के विलय में कई कठिनियां थीं। सेना के भीतर मतभेद और प्रतिरोध मौजूद थे। पटेल ने इस चुनौती का सामना धैर्य और रणनीति के साथ किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी निर्णय केवल राष्ट्रहित के लिए लिया जाएगा, न कि किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए।
क्या होता अगर पटेल प्रधानमंत्री होते?
इतिहासकार मानते हैं कि यदि पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते, तो देश का प्रशासनिक और राजनीतिक परिदृश्य और भी अधिक मजबूत होता। विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नेहरू का अनुभव भी साथ होता। विभाजन और रियासतों का विलय अधिक संतुलित और तेज़ी से होता।
सी. राजगोपालाचारी ने लिखा कि नेहरू विदेश मामलों में दक्ष थे, लेकिन यदि पटेल प्रधानमंत्री होते, तो प्रशासनिक निर्णय और राजनीतिक संतुलन और भी मजबूत होता। यह विचार आज भी इतिहासकारों और नीति विश्लेषकों के लिए महत्वपूर्ण है।
मिथक और वास्तविकता
सरदार पटेल के मुसलमानों के प्रति कठोर होने का मिथक असत्य था। विभाजन और रियासतों के विलय के समय उन्होंने सभी समुदायों के लिए संतुलित निर्णय दिए। उनका दृष्टिकोण केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति और सामाजिक समरसता पर आधारित था। पटेल के सहयोगी अक्सर याद करते थे कि उनकी निर्णय प्रक्रिया में कोई व्यक्तिगत भावना शामिल नहीं होती थी। उनका मंत्र था: देश पहले, स्वयं नहीं। यही दृष्टि आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
आज का भारत और पटेल दृष्टि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार पटेल के कार्य और दृष्टि को उजागर किया। गुजरात के केवड़िया में उनकी विशाल प्रतिमा और उनके परिवार से मुलाकात यह दर्शाती है कि आज का नेतृत्व भी पटेल के आदर्शों और दृष्टि को दोहरा रहा है। राष्ट्रीय एकता, स्थिरता और मजबूत प्रशासनिक ढांचे में उनकी दूरदर्शिता की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। पटेल का योगदान केवल स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था; उनका प्रभाव आज भी भारत की नीतियों और रणनीतियों में दिखाई देता है।
सरदार पटेल ने अपने जीवन में दिखाया कि राष्ट्रसेवा व्यक्तिगत महत्व से ऊपर होती है। उन्होंने सत्ता और पद की महत्वाकांक्षा को पीछे रखकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी। उनके बलिदान और दूरदर्शिता ने भारत को स्थिर, सगठित और अखंड बनाया। नेहरू के “नंबर वन” हठ के आगे झुकना, लेकिन राष्ट्रहित के लिए कदम पीछे लेना, उनकी महानता और आदर्श नेतृत्व को स्पष्ट करता है।
आज भी उनके आदर्श हर भारतीय नागरिक के लिए प्रेरणा हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि एक राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी सेवा केवल पद या शक्ति नहीं, बल्कि बलिदान, दूरदर्शिता और नैतिक नेतृत्व है। जब हम उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं, यह न केवल उनके योगदान को याद करने का अवसर है, बल्कि यह याद रखने का भी समय है कि भारत जैसी स्थिर और अखंड राष्ट्ररचना बनाने के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पीछे रखना ही सच्चा नेतृत्व है।