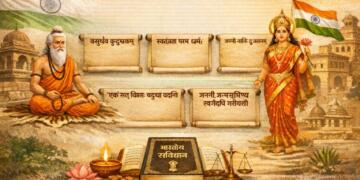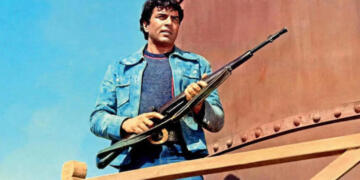खोस्त की सूखी ज़मीन पर जब तालिबानी जवान मंच के चारों ओर खड़े थे और उनके सामने रखा नक्शा पाकिस्तान के कई हिस्सों को अफ़ग़ान मानता दिखा, तो वह केवल एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन नहीं था। वह एक स्पष्ट संदेश था कि काबुल अब पुरानी सीमाओं को चुनौती देने से नहीं हिचक रहा। यह नक्शा, जिसमें ड्यूरंड रेखा को अनदेखा कर पाकिस्तान के कई पश्तून बहुल इलाके शामिल किए गए थे। यह सिर्फ़ कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की सामरिक तंत्रिका को छेड़ने वाला ज्वलंत संकेत था। भारत के लिए यह सिर्फ पड़ोसी के विवाद का मुद्दा नहीं है, यह एक व्यापक, बहु-आयामी सुरक्षा सतर्कता का अलार्म है।
सबसे पहले स्पष्ट कर लें कि यह अभियान केवल पाकिस्तान के लिए शर्मनाक या अपमानजनक नहीं है, यह पाकिस्तान के आंतरिक संकटों और उसकी सैन्य-राजनीतिक रणनीतियों की विफलताओं का औपचारिक खुलासा भी है। जिस देश ने दशकों से अपने पड़ोसी देशों में प्रभाव जमाने के लिए सशस्त्र नीतियों और गुप्त क्रियाकलापों को अपनाया, वही अब काबुल के मंच पर अपने हिस्से का कट दिखते देख रहा है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान की ‘रणनीतिक गहराई’ का मिथक कितनी जल्दी विफल हो सकता है जब स्थानीय परिस्थितियां और पड़ोसी शक्तियां बदल जाएं।
भारत के लिए जरूरी है कदम उठाना
भारत के लिए इस घटना का समग्र अर्थ यह है कि दक्षिण एशिया का परिदृश्य फिर से बदल रहा है और अब निष्क्रिय पर्यवेक्षक बनने का समय गया। पोस्ट-आमेरिकन अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान का यह आत्मविश्वास, पाकिस्तान के भीतर सक्रिय अस्थिर समूहों की वापसी और चीन के आर्थिक-रणनीतिक हस्तक्षेप इन तीनों का जोड़ भारत के सुरक्षा हितों के लिए घातक साबित हो सकता है यदि समय रहते उचित कदम न उठाए जाएं। तालिबान का नक्शा केवल रेखाएं बदलने वाला कृत्य नहीं, वह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो सीमाओं, जनजातीय पहचान और संप्रभुता के संवेदनशील मुद्दों को फिर से उभारता है।
ड्यूरंड रेखा का अस्वीकार पुराने दिनों का पुराना मामला नहीं रहा, वह अब दोनों देशों के बीच बार-बार होने वाली झड़पों, सीमा पार हमलों और हिमायती आंदोलनों की वजह बन सकता है। तालिबान के नक्शे में खैबर पख्तूनख्वा और पश्तून बहुल इलाकों को शामिल कर देना कतई सादा भावनात्मक भाषण नहीं था, यह एक रणनीतिक संकेत था कि तालिबान पाकिस्तान के भीतरी मामलों में अपनी दखलंदाजी का दायरा बढ़ाने के इच्छुक है। इस दावे का तात्त्विक असर यह होगा कि पाकिस्तान के अंदरूनी उथल-पुथल हमारे उत्तर-पश्चिमी सीमाओं पर सीधे महसूस की जाएगी। उधर की अस्थिरता भारत की सीमा-रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिरता को चुनौती देगी।
तालिबान और आईएसआई के संबंधों में दरार
खासकर यह समझना ज़रूरी है कि तालिबान का यह कदम पाकिस्तानी संस्थाओं, विशेषकर ISI के साथ सम्बन्धों की जटिलता को उजागर करता है। वर्षो से चलने वाली चर्चा रही है कि किस हद तक तालिबान और ISI के बीच रैखिक साझेदारी रही है। आज उसमें दरारें भी दिखती हैं। Taliban–ISI के संबंधों में दरार ने क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धा को और पेचीदा बना दिया है, जहां कुछ हिस्से तालिबान को खुले समर्थन देते रहे हैं, वहीं कुछ सैन्य-राजनीतिक फ्रैक्शन चिंतित भी हैं। भारत के लिए इस रिफ्ट का मतलब यह है कि वह समय-समय पर ISI की गलियों में पैदा हुए फूट का इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते उसका इरादा स्पष्ट और प्रभावी हो। परन्तु यह भी सच है कि इस अस्थिरता का लाभ अक्सर सबसे ज़रूरतमंद, समान्य जन और सीमावर्ती समुदाय भुगतते हैं और इससे विस्थापन, शरणार्थी बहाव और आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि का खतरा बढ़ जाता है।
सीपीईसी के स्थायित्व पर भी सवाल
इस पूरे परिदृश्य में चीन की भूमिका एक निर्णायक कारक है। सीपीईसी के माध्यम से चीन ने पाकिस्तान में निवेश कर के न केवल आर्थिक संबंध बनाए बल्कि एक रणनीतिक फ्रंटियर भी स्थापित किया। तालिबान के उदय और अफ़ग़ानिस्तान में उसकी निर्णायक स्थिति, सीपीईसी के स्थायित्व पर प्रश्नचिन्ह लगा सकती है। यदि तालिबान सक्रिय रूप से पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के दावे करता है और वहां अस्थिरता फैला देता है, तो चीन की विशाल परियोजनाएँ—जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए जीवनरेखा हैं, गंभीर संकट में आ सकती हैं। यह स्थिति सीधे चीन के हितों के विरुद्ध है और बीजिंग को या तो तालिबान को नियंत्रण में रखने के लिए पाकिस्तानी नेतृत्व पर दबाव डालना होगा या वह स्वयं किसी और तरह का हस्तक्षेप करने पर विचार करेगा। भारत के लिए यह एक अवसर भी पैदा करता है: चीन और पाकिस्तान के बीच दरारें यदि गहरी हों तो भारत अपनी वैकल्पिक कूटनीतिक चालें मजबूत कर सकता है। पर यह मौका लेने के लिए भारत को सावधान और ठोस रणनीति की आवश्यकता है।
भारत की रणनीति में अब तीन स्पष्ट धुरी शामिल होनी चाहिए—पहला, अपनी खुफिया और सुरक्षा तंत्र की त्वरित पुनरावस्था; दूसरा, क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सक्रिय संघ; और तीसरा, सॉफ्ट पावर का बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल। RAW का अफ़ग़ानिस्तान में बचा हुआ नेटवर्क, उत्तरी गठबंधन के पुराने संपर्क और चाबहार पोर्ट जैसी संरचनाएँ भारत के पास मौजूद हैं, पर इन संसाधनों का प्रभाव तभी प्रभावी होगा जब इन्हें रणनीतिक दृष्टि से सक्रिय किया जाए। चाबहार पोर्ट को केवल व्यापारिक मार्ग के रूप में न देखें; उसे भारत की समग्र रणनीति का एक कार्यशील हथियार माना जाना चाहिए—एक ऐसा रास्ता जो सामरिक कीमत पर भारत को मध्य एशिया और अफ़ग़ानिस्तान तक अपना पहुंच बनाए रखने में समर्थ बनाए। भारत तजाकिस्तान बेस जैसी सुविधाएं भी रणनीतिक गहराई देने का अवसर हैं। इनका प्रयोग reconnaissance, logistics और crisis response के लिए किया जा सकता है।
भारत को करना होगा ये काम
साफ़ है कि केवल कूटनीति बोलने से काम नहीं चलेगा। तालिबान का नक्शा यह संकेत देता है कि प्रत्यक्ष और गुप्त दोनों तरह के उपायों की आवश्यकता है। खुफिया-संचालित कार्रवाई, सीमापार निगरानी, और समय-समय पर गुप्त अभियान को लागू करने की क्षमता को बढ़ाना होगा, पर यह काम अंतरराष्ट्रीय क़ानून और रणनीतिक विवेक के दायरे में रहकर ही करना होगा। यदि भारत गुप्त कार्रवाई के साथ-साथ प्रत्यक्ष राजनयिक दबाव और बहुपक्षीय मंचों में भी सक्रिय रहेगा, तो वह इस तिकड़ी—तालिबान, ISI और CPEC के प्रभाव—को संतुलित कर सकता है।
तालिबान का नक्शा यह भी साफ़ कर देता है कि अफ़ग़ानिस्तान में अब भारत की सॉफ्ट पावर और विकासात्मक पदचिह्न केवल भलाई के काम नहीं रह गए हैं, वे रणनीतिक संकेत बन गए हैं। स्कूल, अस्पताल, बुनियादी ढांचे और लोक-प्रोजेक्ट्स का संरक्षण भारत के लिए अनिवार्यता बन चुका है। यह कार्य केवल मानवीय सहायता नहीं, बल्कि क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और विश्वसनीयता बनाए रखने की रणनीति है। इसके साथ ही भारत-ईरान-अफगानिस्तान गलियारा को मजबूत करना और चाबहार पोर्ट की कार्यक्षमता बढ़ाना अब और अधिक जरूरी हो गया है ताकि भारत अप्रत्यक्ष रूप से अफ़ग़ान बाजार और सामरिक क्षेत्रों तक पहुंच बनाए रख सके।
यह समझना भी आवश्यक है कि भारत को किन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है यदि वह सक्रिय हो जाता है। पहला जोखिम यह है कि पाकिस्तान इसे प्रत्यक्ष उत्तेजना के रूप में देख सकता है और अपने बचाव में और अधिक आक्रामक कदम उठा सकता है, जिससे सीमापार तनाव बढ़ेगा। दूसरा जोखिम यह है कि क्षेत्रीय actors खासकर चीन और कुछ मध्य पूर्वी खिलाड़ी—भारत की सक्रियता को अपने लिए खतरे के रूप में मान कर पाकिस्तान के संरक्षण में और जुड़ सकते हैं। अतः भारत को हर कदम जोड़-तोड़ कर उठाना होगा, और अपने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क—विशेषकर रूस, ईरान, और सेंट्रल एशिया के साथ अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में जोड़ना होगा।
तालिबान के नक्शे के प्रकाशन में एक और चिंता यह है कि आतंकवाद का प्रवाह फिर से नए मार्ग अपना सकता है। अफ़ग़ानिस्तान से हथियार, ट्रेनिंग और कट्टर विचारधारा पाकिस्तान के अंदर और सीमा पार भारतीय क्षेत्रों तक पहुंच सकती है। खासकर जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में यह खतरा गंभीर है। इसलिए भारत को अपनी आतंरिक सुरक्षा प्रणाली, स्थानीय प्रशासन और फॉरेंसिक और मानव-इंटेलिजेंस क्षमताओं को और मजबूत करना होगा। साथ ही सीमावर्ती जिलों में सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं को तेज़ करना होगा ताकि स्थानीय युवा आतंकवादी लॉरी में आकर्षित न हों।
इस नए हालात में भारत के पास कुछ साफ़ विकल्प हैं और हर विकल्प के साथ फ़ायदे और जोखिम जुड़े हैं। पहला विकल्प है डिप्लोमैटिक प्रेशर के ज़रिए पाकिस्तान पर इंटरनेशनल मंचों पर उसकी ज़िम्मेदारियों का मतलब थोपना—लेकिन यह तभी असरदार होगा जब भारत के पास पक्के सबूत और रीजनल सपोर्ट हो। दूसरा विकल्प है खुफिया ऑपरेशन और इंटेलिजेंस-बेस्ड प्री-एम्प्टिव एक्शन—यह जोखिम भरा लेकिन कभी-कभी ज़रूरी होगा; इसमें सावधानी के साथ प्रोपोर्शनैलिटी का पालन करना ज़रूरी है। तीसरा विकल्प है रीजनल अलायंस को मज़बूत करना—रूस, ईरान, सेंट्रल एशियाई देशों और कुछ मामलों में खाड़ी देशों के साथ मिलकर काम करके भारत चीन-पाकिस्तान तिकड़ी के स्ट्रेटेजिक असर को कम कर सकता है। चौथा विकल्प है इकोनॉमिक और सॉफ्ट-पावर पुश—चाबहार पोर्ट की क्षमता और अफगानिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन की कोशिशों को तेज़ करके भारत अपनी लोकप्रियता और असर बढ़ा सकता है।
स्पष्ट होना चाहिए भारत का लक्ष्य
किसी भी विकल्प को अपनाते समय भारत के लिए प्राथमिक लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए: दक्षिण एशिया में स्थिरता और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा। इसका मतलब केवल सैन्य तैयारी नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीति है जिसमें कूटनीति, खुफिया, आर्थिक नीति और मानवीय उपाय शामिल हों। यदि भारत संतुलित, परन्तु निर्णायक नीति अपनाएगा तो वह तालिबान के नक्शे द्वारा बनाए गए मनोवैज्ञानिक दबाव और पाकिस्तान में उठते अस्थिरताओं को नियंत्रित कर सकता है। यदि भारत ने समय रहते कदम न उठाए तो यह नक्शा एक शुरुआत बन सकता है—एक ऐसी शुरुआत जो क्षेत्र में नयी सीमाओं, विस्थापन और हिंसा का मार्ग प्रशस्त कर दे।
एक ठोस तंत्र के रूप में, भारत को तुरंत कुछ कदम उठाना चाहिए। पहला- अपने खुफिया साझा प्रणाली को मजबूत बनाना और पड़ोसी देशों के साथ साझा स्तर पर जानकारी साझा करना। दूसरा- चाबहार बंदरगाह और भारत-ताजिकिस्तान बेस जैश-ए-जाम को परिचालन रूप से तैयार रखना ताकि संकट के समय रसद और सामरिक सहायता दी जा सके। तीसरा- अफगान नागरिक समाज और स्थानीय नेतृत्व के साथ स्थायी संबंध बनाए रखें ताकि भारत पर नरम बिजली प्रभाव बने रहे। चौथा—रक्षा और सुरक्षा के साथ-साथ सीमा पार निगरानी और घुसपैठ विरोधी प्रणाली को उन्नत करना। और पांचवां—अंतरराष्ट्रीय मंचों पर डायनासोर, वृत्तचित्र पर आधारित दस्तावेज़ों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से अलग-अलग तर्क देना।
यह भी ध्यान देना होगा कि तालिबान के नक्शे का असर केवल तत्काल सैन्य या कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं तक सीमित नहीं होगा, यह क्षेत्रीय मानस और स्थानीय पहचान के स्वरूप को भी प्रभावित करेगा। पश्तून समुदायों के लिए यह समय संवेदनशील हो सकता है। उनके बीच तालिबान का संदेश और पाकिस्तान की नीतियां दोनों सामाजिक तनावों को जन्म दे सकती हैं। भारत को इन सामाजिक-राजनीतिक पहलुओं को समझते हुए स्थानीय स्तर पर मानवीय जुड़ाव बढ़ाने चाहिए ताकि भुखमरी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मसलों के ज़रिये हम स्थानीय समर्थन और भरोसा जीत सकें।
आखिरकार, तालिबान का ‘ग्रेटर अफ़ग़ानिस्तान’ का नक्शा भारत के लिए एक वेक-अप कॉल है। यह न केवल पाकिस्तान की सीमाओं पर गहरी लकीरें खींचता है बल्कि दक्षिण एशिया के स्ट्रेटेजिक मैप को भी फिर से परिभाषित करने का संकेत देता है। भारत का कर्तव्य सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना भी है – और इसके लिए उसे सिर्फ passive observer बनने के बजाय सक्रिय, निर्णायक और मल्टी-डाइमेंशनल रणनीति अपनानी होगी। चाबहार पोर्ट, नॉर्दर्न अलायंस से संपर्क, इंडिया-ताजिकिस्तान बेस और RAW जैसे साधन अब सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरत बन गए हैं।
यह समय जरा भी हिचकिचाने का नहीं। यदि भारत ने ठोस और संपूर्ण रणनीति अपनाई, पर covert और overt, कूटनीतिक और सैन्य, विकास और सुरक्षा-तो वह दक्षिण एशिया में अपनी भूमिका और प्रभाव कायम रख सकेगा। वरना तालिबान का यह नक्शा केवल कागज़ पर नहीं रहेगा; यह वास्तविक दुनिया में सीमाओं, जन-जीवन और क्षेत्रीय संतुलन को बदलने की क्षमता रखता है। भारत के लिए अब केवल निर्णय लेना बाकी है-क्या वह जागेगा और सक्रिय होगा, या फिर इतिहास की धूल में एक नया चुनौतीग्रस्त अध्याय बनकर रह जाएगा।