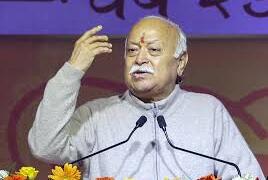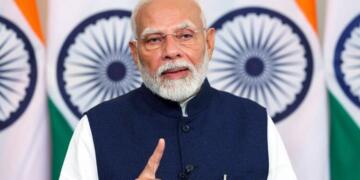26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो भाषण दिया, वह सिर्फ इज़राइल-हमास द्वन्द्व का संदेश नहीं था, वह वैश्विक सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय स्वार्थ की भाषा भी था। नेतन्याहू ने सीधे तौर पर हमास और गाज़ा में रहने वालों को चेताया कि बंधकों को तुरंत छोड़ो, हथियार डालो या परिणाम भुगतोगे। अमेरिका और यूरोप में उठ रहे कूटनीतिक मतभेदों के बीच नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी बाहरी दबाव में अपना सुरक्षा एजेंडा छोड़ा नहीं जाएगा। इस भाषण की एक ही सीधी सीख भारत के लिए है-राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है, और उसे अंतरराष्ट्रीय नैरेटिव से अलग रखकर संचालित करना होगा।
नेतन्याहू ने अपने संबोधन को गाज़ा के भीतर तक पहुंचाने का अनूठा और विवादास्पद कदम उठाया-मोबाइल फोन और बॉर्डर लाउडस्पीकरों पर भाषण का सीधा प्रसारण। यह सिर्फ़ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध और सूचना-संचालन की नई कड़ी थी। भारत के सामने आज वही चुनौती है: जब सीमा पर और आसपास अस्थिरता का माहौल बने, तो केवल सैन्य प्रतिकिये ही काफी नहीं; सूचना, साइबर, खुफिया और मनोवैज्ञानिक युद्ध के आधुनिक आयामों को भी समान रूप से विकसित करना होगा।
भारत की वैश्विक स्थितियों ने हमेशा से देश को सतर्क रखा है। देखिए-पिछले तीन दशक में भारतीय उपमहाद्वीप ने कई बार सशस्त्र संघर्ष, सीमा तनाव और आतंक से जूझा है। इन अनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा और कूटनीति का संतुलन कितना नाज़ुक है। नेतन्याहू ने UN में जो दृढ़ता दिखाई, वह इस सच को रेखांकित करती है कि किसी राष्ट्र के लिए आत्मरक्षा उसका प्रथम कर्तव्य है। भारत के लिए इसका मतलब यही है कि उसकी रणनीति में कठोरता और समझौता-रहितता के बीच संतुलन होना चाहिए — कठोरता जब राष्ट्रीय हितों पर सवाल हो और समझौता तब जब रणनीतिक लाभ मिल रहा हो।
ऊपर के रंगमंच के पीछे जो असली सबक छुपा है, वह यह भी है कि आधुनिक युद्ध केवल थल-समुद्र-व्यवस्था का मैदान नहीं रहा। सूचना युद्ध, खुफिया सेंसर, उपग्रह निगरानी, द्रुत-गति संचार और डेटा-ड्रिवन फैसले अब निर्णायक आते हैं। नेतन्याहू का भाषण उस शक्ति का प्रदर्शन था जो एक राष्ट्र अपनी तकनीकी और इंटेलिजेंस क्षमताओं से कर सकता है- लेकिन भारत को यह सवाल खुद से पूछना होगा कि क्या उसके पास ऐसी समेकित क्षमता है, और अगर नहीं तो उसे तेजी से विकसित क्यों नहीं किया जा रहा है। सीमा पर ड्रोन, रडार और वास्तविक समय की निगरानी पर्याप्त नहीं, स्थानीय स्तर पर सूचना संचलन, मीडियाई नियंत्रण, और मनोवैज्ञानिक परिचालन में भी मजबूती लानी होगी ताकि किसी भी संकट की शुरुआती घड़ी में स्थिति नियंत्रण में रखी जा सके।
राजनीतिक आयामों पर देखें तो नेतन्याहू ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता पर तीखा हमला किया। वह कहना चाहते थे कि किसी भी तरह का ऐसा कदम जो आतंक को पुरस्कृत करे, उसे आत्मघाती ही कहा जाएगा। भारत के लिए यह एक चेतावनी भी है और निर्णय की एक जगह भी। वैश्विक मंचों पर नैरेटिव बदलते रहना सामान्य है, मित्रता और विरोध दोनों समय के साथ बदलते हैं। इसी बदलती जनता-मान्यता के माहौल में भारत को अपना रुख स्पष्ट और सतत रखना होगा-न तो वह केवल अलाइनमेंट्स की राजनीति में उलझेगा और न ही हर वैश्विक दबाव पर झुकेगा। भारत का हित यह है कि वह अपने रणनीतिक फैसलों को घरेलू सुरक्षा और दीर्घकालिक ऊर्जा-ओरिएंटेड नीतियों के साथ मेल कराए।
ऊर्जा और सुरक्षा का नया समीकरण भी इस भाषण से उभरकर आता है। मध्य पूर्व और रूसी तेल पर निर्भरता ने पिछले वर्षों में राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित किया है। नेतन्याहू के निश्चय ने दिखाया कि जब सुरक्षा दांव पर हो, तब ऊर्जा रणनीति भी अचानक भू-राजनीतिक हथियार बन जाती है। भारत को यह समझना होगा कि ऊर्जा की विविधता और आत्मनिर्भरता अब सिर्फ आर्थिक कदम नहीं, बल्कि रणनीतिक ज़रूरत है। यदि किसी भी समय किसी आपूर्ति-स्रोत पर दबाव पड़े तो उसकी भरपाई के उपाय पहले से होने चाहिए – भंडारण क्षमता, वैकल्पिक सप्लायर्स और ऊर्जा दक्षता योजनाएं। इस पर काम कर के ही भारत अपनी विदेश नीति में किसी भी तरह के ब्लैकमेल या दबाव का सामना कर पाएगा।
दूसरी तरफ़, नेतन्याहू का भाषण अमेरिका के साथ रिश्ते पर भी संकेत देता है। अमेरिका जहां एक ओर इज़राइल का करीबी है, वहीं उसकी विदेश नीति में अनियमितताएं और घरेलू राजनीतिक उतार-चढ़ाव अक्सर मित्र देशों के लिए अनिश्चितताएं पैदा करते हैं। भारत के लिए यही समय है कि वह रिश्तों को बहुआयामी बनाए—सिर्फ़ अमेरिकी समर्थन पर निर्भर न रहे। रक्षा, तकनीकी, और खुफिया साझेदारियों को मज़बूत करना जरूरी है, पर साथ ही यूरोप, मध्य पूर्व और पारंपरिक साझेदारों के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक विकल्पों को भी विकसित करना होगा। बहुध्रुवीय दुनिया में भारत को अपनी संप्रभुता बरकार रखने के लिए कई द्वार खोलने होंगे, न कि एक ही पर अपनी तक़दीर बांधकर बैठना होगा।
घरेलू स्तर पर भी इस भाषण का प्रभाव देखने लायक होगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में मानवाधिकार, युद्ध की नैतिकता और नागरिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना कठिन होता है। नेतन्याहू ने UN की सभा में जो कड़े शब्द बोले, वे यह दर्शाते हैं कि जब राष्ट्रीय अस्तित्व का सवाल उठता है तो सरकारें कठोर कदम उठाने को तैयार होती हैं। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी कार्रवाईयां कानूनी, नैतिक और रणनीतिक दृष्टि से मजबूत हों। साथ ही, सार्वजनिक संचार नीति को भी इतनी प्रभावी बनाना होगा कि गलतफहमियों और वैकल्पिक नैरेटिव से देश की एकता और सेना-प्रशासन की वैधता पर हमला न हो सके।
क्षेत्रीय समीकरणों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इज़राइल-हमास संघर्ष से मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ेगी और उससे भारत के ऊर्जा, प्रवासी नागरिकों की सुरक्षा, और व्यापारिक मार्गों पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत के अरब साझेदारों के साथ आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते हैं; इसलिए दिल्ली को अपनी बातचीत और कूटनीति में सावधानी बरतनी होगी, ताकि वह अपनी आर्थिक जरूरतें और सामरिक हित दोनों बराबरी से संभाल सके। विदेश नीति के इस संकुल में सोच-समझ कर कदम उठाना ही भारत की मजबूती होगी।
अंततः, नेतन्याहू के भाषण ने एक बात और स्पष्ट कर दी: आधुनिक संघर्ष केवल बंदूकों और बमों तक सीमित नहीं रहा। नैरेटिव, वैश्विक सहानुभूति, और मानवीय-वैश्विक कानून इन हरकतों का हिस्सा हैं। भारत को इन सभी आयामों में चुस्त होना होगा — सैन्य बल के साथ कूटनीतिक मसल और वैश्विक मंचों पर अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने की क्षमता तभी काम आएगी जब देश की हुकूमत, सेनाओं और तकनीकी तंत्र एक ही दिशा में काम करें।
इस पूरे मोर्चे पर एक निर्णायक आग्रह यह भी है कि भारत को अपनी रणनीति में दीर्घकालिक सोच को अपनाना होगा। जल्दबाज़ी के राजनीतिक निर्णय, झटपट समझौते या भावनात्मक कदम अक्सर राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाते हैं। नेतन्याहू ने UN में जो दृढ़ संदेश दिया, वह इस बात का परिचायक है कि जहां सुरक्षा का प्रश्न है, वहां उठापटक से काम नहीं चलेगा। पर साथ ही यह भी याद रखना होगा कि सैन्य जीत के बाद भी स्थिरता तब तक नहीं आएगी जब तक राजनीतिक और सामाजिक समाधान न निकल आएं। इसलिए भारत को न सिर्फ रक्षा की परिपक्वता दिखानी है, बल्कि उसका सामाजिक और कूटनीतिक आशय भी मजबूत बनाना है।
नेतन्याहू के भाषण की उपलब्धियों और सीमाओं दोनों से भारत को सीखने की गुंजाइश मिलती है। उपलब्धि यह कि उसने वैश्विक मंच का प्रयोग कर के स्पष्ट संदेश दिया, सीमा यह कि भाषण और धमकी अकेले किसी गहरे और दीर्घकालिक समस्या का हल नहीं दे सकते। भारत के लिए समाधान का मार्ग स्पष्ट होना चाहिए — सुरक्षा-प्राथमिकता के साथ टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस को ऊंचा स्थान देना, ऊर्जा और आर्थिक स्वायत्तता को मजबूती देना, बहु-धुरीय कूटनीति को जीवन्त बनाए रखना, और अंततः देश की एकता और संस्थाओं की ताकत को बनाए रखना।
यह समय है देशाभिमानी ठोस नीतियों का, तेज़ परिकल्पनाओं का और धैर्यपूर्ण परिश्रम का। नेतन्याहू का UNGA भाषण हमें याद दिलाता है कि जो राष्ट्र अपने हितों के लिए स्पष्ट और दृढ़ रहता है, वही कठिन दौर में सुरक्षित रह पाता है। भारत ने अब तक कठिनाइयों का सामना किया है और निकला भी है। इस नई वैश्विक चुनौती के समय भी भारत को वही साहस, वही दूरदर्शिता और वही आत्मनिर्भरता दिखानी होगी — भाषणों के नहीं, कारवाईयों के जरिए।