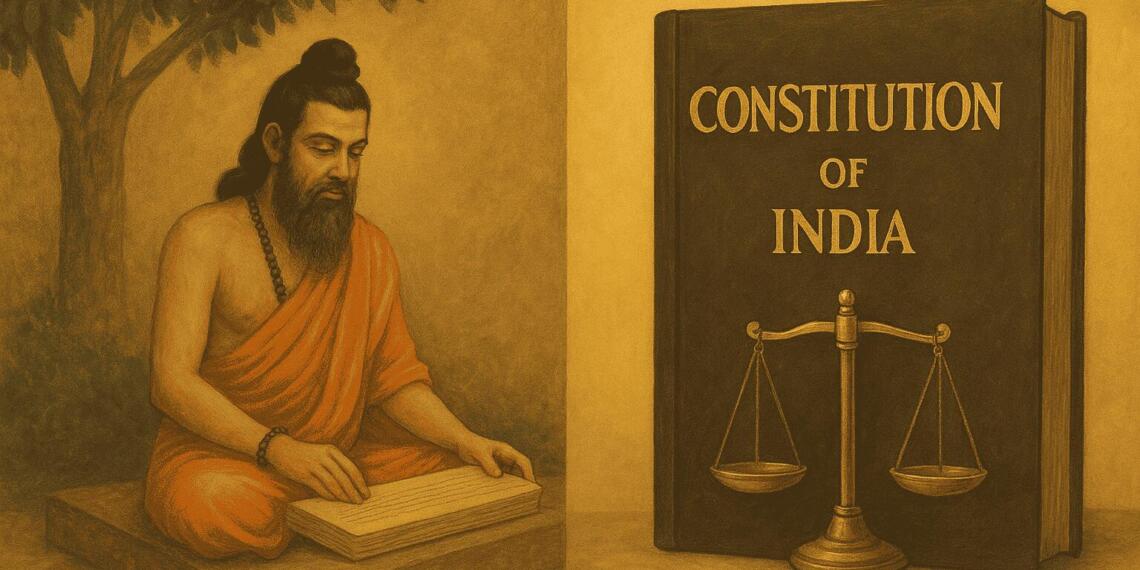भारतीय ज्ञान परंपरा में नागरिकता (Citizenship) का विचार आधुनिक “राज्य–नागरिक” (State–Citizen) ढाँचे से भले अलग रहा हो, पर इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और बहुआयामी है। भारतीय संविधान का भाग–2 (नागरिकता) मूलतः भारतीय ज्ञान परंपरा की उस व्यापक और नैतिक दृष्टि का आधुनिक संवैधानिक रूप है, जिसमें नागरिकता केवल कानूनी पहचान नहीं, बल्कि कर्तव्य, आचरण, सामूहिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र–हित से जुड़ी गहन सामाजिक व्यवस्था है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एकात्म राजधर्म, अहिंसा एवं समता आधारित नागरिक जीवन, प्रजा–कल्याण का अर्थशास्त्रीय मॉडल, तथा कर्तव्य–प्रधान सामाजिक संरचना, ये सभी तत्व संविधान की एकल नागरिकता, समता, सुरक्षा और नैतिक दायित्व की अवधारणा में जीवित हैं। इस प्रकार संवैधानिक नागरिकता भारत की प्राचीन दार्शनिक परंपराओं को आधुनिक लोकतांत्रिक ढाँचे में प्रतिष्ठित करती है।
वैदिक युग और नागरिकता की अवधारणा
वैदिक युग में ‘जन’ आधारित समुदायिक नागरिकता की अवधारणा दिखाई पड़ती है। वैदिक साहित्य में नागरिकता का विचार जन, जनपद, नर, विश, सभा, समिति जैसे शब्दों में मिलता है। व्यक्ति की पहचान राज्य की नागरिकता से ज़्यादा समुदाय, कुल, ऋत और धर्म के पालन से निर्धारित होती थी। ऋग्वेद में “जनस्य रक्षक” (जन के रक्षक) और “जनस्य गोप्ता” (समुदाय के संरक्षक) जैसे पद नागरिक राज्य संबंध को दर्शाते हैं। भारतीय नागरिकता की विशेषताएँ सामूहिक निर्णय–प्रक्रिया, कर्तव्य–प्रधान व्यवस्था, और प्राकृतिक न्याय व ऋत के अनुरूप जीवन पर आधारित हैं।
भारत के संविधान का भाग 2 भी नागरिकता के संबंध में इसी प्रकार का विचार रखता है। संविधान के अनुसार नागरिकता केवल कानूनी स्थिति नहीं, बल्कि नैतिक उत्तरदायित्व भी है।
राज्य और नागरिक दोनों “संवैधानिक धर्म” का पालन करते हैं जो भारतीय परंपरा में “राजधर्म” के रूप में मौजूद था। (ऋग्वेद 1.89.1, 10.191) इन ऋचाओं में समूहिक निर्णय एवं अनुशासन की अवधारणा को विस्तार से वर्णन किया गया है। उपनिषदों में नागरिकता राजनीतिक न होकर नैतिक बन जाती है।
व्यक्ति को विश्व–नागर (Cosmic citizen) के रूप में देखा गया है। ईशावास्योपनिषद: “तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा” के माध्यम से उपभोग में संयम का सिद्धांत, और इसे नागरिक – कर्तव्य का आधार माना गया। छांदोग्य उपनिषद में सत्य, अहिंसा, दान, स्वाध्याय को सामाजिक जिम्मेदारी कहा गया है और सभी से अपेक्षा की गयी है कि इसके अनुसार आचरण करते हुये समाज को आगे बढ़ाते रहे।
प्रचीन भारत में नागरिकता का संदर्भ
महाकाव्य काल जैसे महाभारत और रामायण युग में नागरिकता केवल अधिकारों का संबंध नहीं थी, बल्कि राजा और प्रजा दोनों के परस्पर कर्तव्यों पर आधारित एक नैतिक सामाजिक व्यवस्था थी। महाभारत के शांतिपर्व में राजा के सर्वोच्च गुण के रूप में “प्रजावत्सलता” का उल्लेख किया गया है, जिसमें शासक को अपनी प्रजा की रक्षा, पोषण और कल्याण उसी प्रकार करना चाहिए जैसे माता–पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार रामायण में “प्रजा सुखे सुखं राज्ञः”, यह सिद्धांत स्थापित किया गया है कि राजा का सच्चा सुख प्रजा के सुख में ही निहित है। इसी परंपरा का आधुनिक और कानूनी रूप भारतीय संविधान के भाग–2 (नागरिकता) में दिखाई देता है।
भाग–2 नागरिकता को केवल कानूनी स्थिति मानते हुए भी उसके केंद्र में राष्ट्र के प्रति निष्ठा, संवैधानिक कर्तव्यों और सार्वजनिक हित को रखता है। महाकाव्यकाल की तरह यहाँ भी नागरिकता का उद्देश्य यह है कि नागरिक और राज्य दोनों एक–दूसरे की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण में संलग्न रहें। इस प्रकार महाभारत और रामायण का “कर्तव्य–प्रधान नागरिकता” दृष्टिकोण, संविधान के भाग–2 में “कानूनी नागरिकता” के भीतर छुपी उस मूल भावना को उजागर करता है, जिसमें राष्ट्र, राज्य और नागरिक तीनों एक – दूसरे के कल्याण से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं।
बौद्ध संघ की वोटिंग, सभा और बहुमत–आधारित व्यवस्था नागरिकता में सहभागिता, अनुशासन और समानता की भावना है, जो आधुनिक संविधान में नागरिक के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अनुरूप है। विनय पिटक में वर्णित संघ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया नागरिकता को केवल कानूनी पहचान नहीं, बल्कि सामूहिक निर्णय और नैतिक जीवन से जोड़ती है। जैन दर्शन के अहिंसा, अपरिग्रह और समता के सिद्धांत नागरिकता को नैतिक संयम, सामाजिक सद्भाव और सभी के प्रति न्यायपूर्ण दृष्टि प्रदान करते हैं। इस प्रकार संविधान का भाग 2 जहाँ नागरिकता का विधिक ढाँचा देता है, वहीं बौद्ध–जैन परंपराएँ उसकी नैतिक आत्मा को मजबूती देती हैं।
कौटिल्य नागरिकता को केवल शासित और शासक के संबंध तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे राज्य–व्यवस्था के केंद्र में स्थापित करते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रजा “स्वामी के समान मूल्यवान” है, अर्थात् नागरिकों का हित और सुरक्षा सर्वोच्च शासन–धर्म है। अर्थशास्त्र में नागरिकों की रक्षा, आजीविका का प्रबंध, व्यापार की स्वतंत्रता और निगरानी, शिक्षा की उपलब्धता तथा न्याय की सुलभता को राज्य की अनिवार्य जिम्मेदारियों में गिना गया है। कौटिल्य के अनुसार नागरिकता (प्रजा–स्थिति) पाने का आधार जन्म, राज्य की स्वीकृति, राज्य के नियम–पालन, कौशल या पेशे के आधार पर स्वीकार्यता, तथा कर और कर्तव्यों का पालन था अर्थात जो राज्य की सुरक्षा स्वीकार करे और उसके नियमों का पालन करे, वही नागरिक माना जाता था।
गुप्त, मौर्य और अन्य प्राचीन भारतीय राज्यों में नागरिकता का स्वरूप औपचारिक कानून के बजाय सामाजिक स्वीकार्यता, स्थानीय संस्थाओं में सहभागिता और राज्य–सुरक्षा पर आधारित था। इन कालों में नागरिकता प्राप्त करने का प्रमुख आधार जन्म, स्थायी निवास और किसी नगर, ग्राम या गिल्ड (श्रेणी) का मान्य सदस्य बनना था। व्यापारी, कारीगर और शिल्पकार जब किसी गिल्ड में शामिल होते थे, तो उन्हें उस गिल्ड के संरक्षण, नियमों और न्याय–व्यवस्था के माध्यम से नागरिक अधिकार प्राप्त होते थे। जो व्यक्ति राज्य को कर देता, सामुदायिक दायित्व निभाता और राज्य के नियमों का पालन करता, उसे पूर्ण ‘प्रजा‘ यानी नागरिक माना जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत में नागरिकता जन्म, निवास, पेशागत समूह की सदस्यता और राज्य–सुरक्षा—चारों के सम्मिलित आधार पर स्थापित होती थी।
मध्यकालीन भारत में नागरिकता का स्वरूप समुदाय आधारित, सहमति प्रधान और स्थानीय प्रशासन पर आधारित दिखाई देता है। इस समय गाँवों और नगरों में पंचायतें न्याय, प्रशासन, विवाद–निराकरण और सामाजिक व्यवस्था का संचालन करती थीं। पंचायतें केवल प्रशासनिक संस्थाएँ नहीं थीं, बल्कि वे नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के निर्धारण का मुख्य आधार भी थीं। इनके निर्णय सामूहिक सहमति से लिए जाते थे, जिससे नागरिकता का स्वरूप स्थानीय सहभागिता और सामुदायिक जिम्मेदारी पर आधारित बनता था।
आधुनिक भारत में नागरिकता औपनिवेशिक मन:स्थिति से निकलकर संविधान के भाग 2 (नागरिकता) के माध्यम से एक स्पष्ट, अधिकार–आधारित और लोकतांत्रिक स्वरूप धारण करती है। स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा स्थापित स्वराज, स्वतंत्रता, समानता और सक्रिय सार्वजनिक सहभागिता के सिद्धांत अब संवैधानिक नागरिकता की नींव बनते हैं। संविधान के भाग 2 के अनुसार नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और क्षेत्र के शामिल होने के आधार पर निर्धारित होती है। यह वही विचार है जो स्वतंत्रता संग्राम की व्यापक एवं सहभागी नागरिकता–दृष्टि को कानूनी रूप देता है। इस प्रकार आधुनिक काल में भारतीय नागरिकता नैतिकता, भागीदारी और अधिकार के पारंपरिक मूल्यों को संवैधानिक ढाँचे में स्थापित करती है। ये सभी मूल्य भारतीय चिंतन परंपरा की ही अभिव्यक्ति हैं।
डा. आलोक कुमार द्विवेदी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दर्शनशास्ञ में पीएचडी हैं। वर्तमान में वह KSAS, लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। यह संस्थान अमेरिका स्थित INADS, USA का भारत स्थित शोध केंद्र है। डा. आलोक की रुचि दर्शन, संस्कृति, समाज और राजनीति के विषयों में हैं।